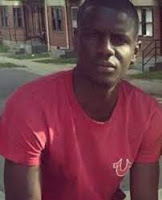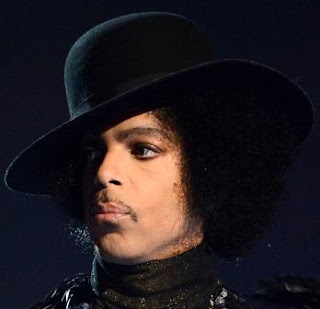संतोष कुमार चतुर्वेदी की नयी कविताएँ, अनुनाद के पाठकों के लिए। हां, इनमें सांसद/विधायक सीट वाली कविता इससे पहले पहल में छप चुकी है और सराही भी गई है। ज़्यादातर पाठक जानते हैं कि संतोष अनहदनाम से एक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन-सम्पादन करते हैं। पहली बारउनका लोकप्रिय ब्लॉग है। संतोष को मैंने इन दोनों ही प्रकाशन माध्यमों के लिए बहुत मेहनती पाया है। पत्रिका के लिए स्तरीय सामग्री जुटाना बहुतायत के इस दौर में बुरा बनने की हद तक कठिन और जोखिमभरा कार्य है। विडम्बना यह भी कि हमारे वक़्त का एक प्यारा और ज़रूरी कवि इस काम में लगातार पीछे छूटता जाता है, जिसके लिए संतोष के मन में कोई मोह कभी नहीं उपजता, टीस शायद उठती हो। ऐसा होना अच्छा ही है, आत्मप्रचार और आत्ममुग्धता के अनगिन छोटे-छोटे टापुओं पर खड़ी कविता को ऐसे ही निर्मोही कवियों की ज़रूरत है, जो किसी टापू पर खड़े न रहकर पूरी विनम्रता के साथ जनता और उसकी भाषा के समूचे धराधाम पर रहना चाहते हैं।
अनुनाद पर संतोष का स्वागत और इन कविताओं के लिए सम्पादक की ओर से आभार।
***
चोरिका
माँ बताती थी हमें अक्सर यह बात कि
प्यास को महसूसने वाले ही
जानते हैं प्यास की महत्ता को
भूख का दंश भुगतने वाले ही
पहचानते हैं अनाज के मर्म को
बाकी तो महज लफ्फाजी करते हैं
माँ भूख-प्यास के सरगम से वाकिफ थी भलीभांति
इसलिए उसने नखलिस्तान की दुर्गम लय पर गाना सीखा था
आज भी वह शीशे के टुकडे पर सहजता से नाचती दिख जाती थी
इस बात की परवाह किये बिना कि
लहुलुहान हो सकती है वह किसी भी क्षण
एक गृहिणी थी माँ
और इसी नाते कहा जा सकता है यह कि
उसकी अपनी कोई कमाई भी नहीं थी
दिन-रात उसके खटने को
श्रम की फेहरिस्त से सदियों पहले ही गायब किया जा चुका था
जैसे गौरैया ने बनाया अपना खोंता
और एक भी तिनका कम नहीं पड़ा कहीं
जैसे मधुमक्खियों ने लिए मकरन्द
और फूलों की महक और बढ़ गयी
जैसे धूप ने पिया चुल्लू भर-भर कर पानी पूरे दिन
फिर भी धीमा नहीं पड़ा नदियों का प्रवाह
वैसे ही माँ ने चोरिका बचाया
और कहीं भी कुछ कम नहीं पड़ा
माँ गृहिणी थी
फिर भी आपद-विपत में जब-जब पड़े कमासुत पिता
तो मजबूती से साथ खडी नजर आयीं माँ ही हमेशा
जब भी गाढ़ा वक्त आया
काम आया माँ का चोरिका
घर ने राहत की साँसे लीं भरपूर
हमारी जिंदगी का रंग थोडा और गाढ़ा हुआ
मिट्टी की उर्वरता पर
हमारा भरोसा थोडा और पुख्ता हुआ
पड़ोसियों की सख्त जरूरतों के समय
फुहारों की तरह दिखा चोरिका
दरवाजे से कोई भूखा वापस नहीं लौटा कभी
मोहल्ले भर की बेटियों के लिए
सौगातें ले कर आया यही
फिजूलखर्ची से जद्दोजहद की महक थी इसमें
अपनी जरूरतें कमतर करने की सनक थी इसमें
औरों को भी खुशहाल देखने की बनक थी इसमें
कमाई का तनिक भी अहम नहीं था
फिर भी श्रम था यह
चोरी का रंच मात्र भी आशय नहीं था कहीं इसमें
फिर भी यह चोरिका था
जिसे माँ ने बड़े जतन से बचाया था
खस्ताहाल दिनों के लिए
गुरुत्व
इस ब्रहमाण्ड में जो भी पिण्ड हैं
सभी का अपना एक गुरुत्व है
इस गुरुत्व के दम पर ही
सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, मंगल सबका
अपना-अपना ओहदा है
स्वार्थों का गुरुत्व भी
खींचता रहता है लगातार अपनी तरफ हमें
किसिम-किसिम के लुभावनकारी गुरुत्वों में
खो जाते हैं अनायास ही हम
अपना अस्तित्व गँवा कर
कोई भी प्रलोभन छोड़ पाना हमेशा मुश्किल होता है
ओहदा ठुकराना और भी मुश्किल
जिगर वालों में से भी
बिरले ही कर पाते हैं ऐसी हिमाकत
लेकिन जो भी छोड़ने का साहस दिखाते हैं
जो भी मर-मिटने के खतरे उठाते हैं
वही गुरुत्व की सरहद तोड़ पाते हैं
वही जा पाते हैं सुदूर अन्तरिक्ष की गहराईयों में
कूड़ा-करकट
यह जो ढेर है दुर्गन्धयुक्त
देखने में भद्दा और अशोभनीय
छाडन हैं हमारी ही मुख्य धाराओं के
यहाँ पड़े हैं जो चिरकूट- चिथड़े
वे हमारे ही कपड़ों के अवशिष्ट हैं
यहीं पड़े हैं वे सपने
जो अरसे तलक देखे जाने के बावजूद
पूरे नहीं हुए कभी
बन न सके अपने
यहीं दबी पड़ी हैं हमारी वे रुचियाँ
जो हमारी जरूरतों के जद्दोजहद में
गुम हो गयीं कहीं
यहीं बिखरे पडे हैं वे कागज़
जो लिखे जाने के बावजूद
फाड़ डाले गए चिन्दी-चिन्दी
यहीं विस्मित पड़े हैं वे पम्फलेट
जो बिन पढ़े ही फेंक डाले गए
यहाँ की अमानत हैं खाली बोतलें और शीशियाँ
जिनमें कभी मौके पर जीवन बचाने की
सुघड़ कहानियाँ भरी थीं
हल्दी, मसाले, मिर्च, धनिया, नमक के वे खाली पैकेट
जिनमें कभी स्वाद के बेशुमार गीत भरे थे
पड़े हैं यहाँ पर
उन बल्बों ने भी पाया है यहीं पनाह
जो अनेक अँधेरी रातों को उजियार बनाते हुए
अब फ्यूज हो चुके हैं
कूड़ा-करकट का यही ढेर
काम आया तमाम खाईयों को भरने में
शहर की नामचीन इमारतों की चौपाईयाँ
गढ़ी गयीं इन्हीं की मात्राओं पर
पुराविदों ने पढ़ीं अतीत की कई लिपियाँ
नष्ट-भ्रष्ट हो चुके
कूड़ा-करकट बन चुके ढेर से
जहां से शिष्ट लोग नाक दबा कर गुजरते हैं
वहीँ तमाम बच्चे
सुबह से शाम तक
अपनी उम्मीदें बटोरतें हैं
कूड़ा-करकट के इस भीमकाय ढेर में
व्यर्थ चीजों के बीच से ही
मिल जाती हैं अनमोल चीजें अक्सर
व्याकरंणविदों को भी मालूम है
कि अर्थहीन होने के बावजूद
निरर्थक शब्द एक लय रचते हैं
टेलीफोन डाईरेक्टरी
कभी इसमें शामिल होने का एक ख़ास मतलब हुआ करता था
हजारों नामों के बीच महीन अक्षरों में लिखा अपना नाम, पता और
टेलीफोन नंबर देख कर लोग रोमांच से भर जाते थे
महीन से महीन अक्षर भी इतना बड़ा लगता था
जैसे वह शामिल हुए की कद-काठी से बड़ा हो जाता था
टेलीफोन डाईरेक्टरी में शामिल लोग
गर्व से बताते फिरते थे इस उपलब्धि के बारे में उन लोगों को
जो इससे प्रायः गैरहाजिर ही रहते आये थे
घर आये आगंतुकों को दिखाया जाता जरुरी तौर पर वह पृष्ठ
जिस पर यह जानकारियाँ छपी होती थीं
एक जमाने में स्टेट्स सिम्बल थी
आज जीवाश्मों की तरह ही बची हैं ये टेलीफोन डाईरेक्टरियाँ
समय बीता और अब तो हर हाथ आ गए मोबाईल
यही नहीं हर अंगुली तक का अब अपना नम्बर
आखिर कोई कहाँ तक शामिल करता इन नंबरों को किसी टेलीफोन डाईरेक्टरी में
लेकिन बात यही नहीं महज
कुलीनों को भला कैसे बर्दाश्त होता उनका साथ
जो जाने जाते हैं आज भी ठेले वाले, कबाड़ी वाले और सफाई वाले के नाम से
उनके नाम भी तो उनके लिए इतने अस्पृश्य कि
उनसे संक्रमित होने का खतरा बना रहता बराबर
लेकिन इसकी परवाह उन्हें कहाँ जो लम्बे अरसे तक उगाते रहे अपने खेतों में बाँस
इसकी खबर उन्हें कहाँ जो कारखानों के दमघोटूं माहौल में आजीवन बनाते रहे लुगदी
और जिनकी सारी सफेदी करीने से चुरा ले गया कागज़
इसकी परवाह उन्हें भी कहाँ जो स्याही की कालिख से लगातार बने रहे बदरंग
और उनके हाथों की बनी स्याही रोशनाई बन कर चमकती-दमकती रही कागज़ पर
नाम, पते और नम्बर के रूप में
अब उन सबके हाथों में नंबर है बिल्कुल अपना
जिससे वे देश-दुनिया की बातें करते हैं धड़ल्ले से
इस से बेफिक्र हो कर कि
किसी जमाने में एक टेलीफोन डाईरेक्टरी भी हुआ करती थी
वह टेलीफोन डाईरेक्टरी अब दफ्न है अपने कब्र में
जिस दुनिया में तमाम विशेषाधिकार सिमट जाते हैं महज कुछ लोगों में
जिस दुनिया की डाईरेक्टरी में जब अंट पाते हैं कुछ चुनिन्दा नाम ही
उन्हें जीवाश्म बनने से नहीं रोका जा सकता
वह दुनिया तब्दील हो ही जाती है टेलीफोन डाईरेक्टरी में
आखिरकार एक दिन
पासंग
पत्थर का यह छोटा सा टुकड़ा
जो तराजू के एक पलड़े पर
मौजूद रहता है हमेशा
बटखरे के बगल में
अपने-आप में कोई बटखरा नहीं
जब तराजू के पलड़े असन्तुलित हो
बेमानी करने लगते हैं
बटखरे भी जब उद्धत हो मनमानी करने लगते हैं
तब यह पासंग ही होता है
जो आगे बढ़ कर रोकता है
इनकी बेमानी-मनमानी
अपने-आप में इनका कोई तय आकार नहीं कोई आकृति नहीं
अपने-आप में इनकी कोई निश्चित तौल नहीं
खराब पड़ी टार्च-बैटरी या ईंट-पत्थर के टुकडे भी बन सकते हैं पासंग
अपने निहायत छोटे आकार-प्रकार में भी
ये तौल को एक तुक-ताल में ढालते हैं
पस्त पड़ चुके सच में फिर जान डालते हैं
और बेराह हो चले जमाने को ढर्रे पर लाते हैं
बेरंग पड चुकी जिंदगी में
बार-बार भरते हैं उल्लास के रंग
यही बेरूप-बेआकार पासंग
परिवहन निगम की बस में सांसद-विधायक सीट
परिवहन निगम की बस में यात्रा करते हुए आपने भी देखा होगा
कि एक समूची सीट के उपर दर्ज होता है यह
‘माननीय सांसद/विधायक के लिए’
इतने दिनों की यात्रा में मुझे कभी नहीं दिखाई पड़े कोई माननीय
बस में अपने लिए आरक्षित सीट पर बैठ कर यात्रा करते हुए
परिचितों ने भी नहीं देखा कभी यह अजूबा
फिर किस बाध्यता के तहत जारी है यह पाखण्ड आज तलक?
क्या यह मखौल नहीं है इस देश की जनता के साथ
जिसे इस भ्रम के साथ जिन्दा रखा जाता है
कि हो सकता है कि कभी कोई माननीय आ ही जाए
और उन पर सनक सवार हो जाय बस यात्रा की
जबकि सबको पता है यह सच्चाई
कि आज का एक ग्राम-प्रधान भी चुनाव जीतने के बाद
लक्जरी गाड़ियों से ही चलना पसंद करता है
फिर माननीय तो ठहरे माननीय
उनका क्या कहना
पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर बस में आते हैं यात्री
और पूरे इत्मीनान से बैठ जाते हैं उस सीट पर
जो माननीय के नाम पर दर्ज होती है
उसे पता होती है यह बात कि अगर गाहे-बगाहे आ ही गया कोई माननीय बस में
तो उसे तत्काल ही खाली करनी पड़ेगी वह सीट
लेकिन उसे यह भी पता है कि ऐसी अनहोनी संभव ही नहीं
भले ही दूध से पानी की एक-एक बूँद को अलगा दिया जाय
और चलनी में से एक भी बूँद पानी न गिरे
चलिए, एक मिनट के लिए मान ही लेते हैं
कि भूले-भटके आ ही गया अगर कोई माननीय बस में
तो एकबारगी बस में बैठा कोई भी यात्री यकीन न कर पाएगा
और पूरे भरोसे के साथ उनके माननीय होने पर सन्देह करेगा
हो सकता है बस के समूचे यात्री उन्हें कोई फरेबी समझे
और उन्हें उतार दे जबरिया बस से तत्काल ही
और अगर बैठ ही गए माननीय किसी तरह अपनी सीट पर
तो पूरे रास्ते लोग उनके बचकानेपन की खिल्ली उड़ाएँ
और फुसफुसाते हुए ही सही ये बाते करें आपस में
कि कैसा सांसद-विधायक है यह बेचारा
जो आज तक अपने लिए एक गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर सका
वह अपने क्षेत्र की जनता के लिए व्यवस्था क्या ख़ाक कर पायेगा
लेकिन यह भी क्या मानना कि माननीय आएंगे
और निहायत अकेले होंगे
उनके साथ न तो कोई अंगरक्षक होगा
न ही कोई समर्थक या फ़ौज-फाटा
हो सकता है कि वे जब सदल बल आएँ तो उनके लिए पूरी बस भी पर्याप्त न पड़े
और भीड़ इतनी हो कि उनके साथ के अति महत्वपूर्ण लोगों को खड़े-खड़े यात्रा करनी पड़े
इसलिए इस सोच के फलीभूत न होने में ही भलाई है बस यात्रियों की
बसें केवल यात्रियों को ढोने के लिए हैं
और ध्यान रहे यह
कि माननीय यात्रा करते हुए भी यात्री नहीं होते कभी
वे सिर्फ और सिर्फ माननीय होते हैं
इसलिए वे बस में नहीं चलते कभी
यही तो करिश्मा है हमारे लोक तंत्र का
कि लोक अलग रहता है तंत्र अलग
दोनों चुनाव के वक्त बेर-केर की तरह एक जगह होते हैं महज दिखावे के लिए
बाकी समय लोक जद्दोजहद करता है
और तन्त्र अय्यासियों में लीन रहता है
अब बस यात्रियों को ही ले लीजिये
जो कंडक्टरों और ड्राईवरों की मनमानी में
अभिशप्त होते हैं पूरे का पूरा किराया चुका कर खटारा बसों में
पसीने से लथपथ हो समय-कुसमय चलने के लिए
जबकि यह जानने के बावजूद कि
भूलकर भी नहीं करता कोई माननीय
आज के समय में बस से चलने की भूल
उनके नाम बिलावजह आरक्षित कर दी जाती है एक पूरी सीट
क्यों न माननीयों के लिए जरुरी कर दिया जाय कि
वे भी अपनी कुछ यात्राएँ करें आम लोगों की तरह ही
टिकट कटाएँ अपनी जेब से पैसे दे कर
बस भरी होने पर खड़े हो कर यात्रा करें
ताकें आम लोगों की तरह ही
कि कौन सी सीट खाली होने वाली है अगले मुकाम पर
और फिर उस पर बैठने की जुगत करें
बकाया रूपया मांगने पर कंडक्टर खुदरा न होने का बहाना बना कर
डकार जाए बाकी सारा रूपया
मैं पूरे मन से मनाता हूँ
कि माननीय की इस बस यात्रा में बस एकाध बार पंक्चर जरुर हो
और घुर्र घुर्र कर के रास्ते में दो चार बार रुके जरुर
फिर धकेलना पड़े बस को तभी चले वह आगे
यात्रा करते हुए घिर आये रात और बस के सामने के बल्ब जले ही ना
माननीय को खाने पड़ें हिचकोले औरों की तरह ही
और उन्हें पता चले कि जो सड़क
उनके परिजनों ने सांसद निधि के कोटे से ठेके पर बनवाई थी
उसका नामो निशान ही नहीं कहीं अब
कि यह तो बस के बस की ही बात है
कह लीजिए बस का ही करिश्मा है
जो गड्ढों को भी अपना रास्ता बनाते हुए चलने का दुःसाहस कर पा रही है
एक कवि होने के नाते
अपने तमाम तकलीफदेह बस यात्राओं के अनुभव के आधार पर
अपनी जनता के पक्ष में लोकतन्त्र के भरोसे के लिए
इस तरह सोचने का जोखिम उठाता हूँ
यह जानते हुए भी
कि माननीयों के बारे में ऐसा सोचना भी
ताजिकिराते हिन्द की किसी न किसी दफ़ा के अंतर्गत
संगीन जुर्म की श्रेणी में जरुर आता होगा
***