(अपनी इजा, कोजेड़ज्या, काकियों और अपनी भौजियों को जो जिन्दा है और उन आमाओं को जो पहाड़ जीते हुए शहीद हो गयीं - उनको जिन्होंने पहले पहल मुझे हिमालय दिखाया)
१-
पहाड़ों पर नमक बोती औरतें
बहुत सुबह ही निकल जाती हैं
अपने घरों से
अपने घरों से
होती है तब उनके हाथों में
दराती और रस्सी
चूख1के बड़े-बड़े दाने
सिलबट्टे में पिसा गया
महकदार नमक
दराती और रस्सी
चूख1के बड़े-बड़े दाने
सिलबट्टे में पिसा गया
महकदार नमक
छोड़ आती हैं वे बच्चों की आँखों के भीतर
सबसे मीठी कोई चीज
सबसे मीठी कोई चीज
लेकिन नहीं होती वे पर्वतारोही
दाखिल होते हैं पहाड़ अनिवार्यताओं के साथ
उनके जीवन में
दाखिल होते हैं पहाड़ अनिवार्यताओं के साथ
उनके जीवन में
हर दिन पहाड़ों को पाना होता है
उनसे पार
उनसे पार
उनके पास होता है तेज चटपटा नमक व गुड़ भी
जिसे खर्चती हैं वे मोतियों की तरह
किसी धार2पर
ढलान में उतरते हुए या फिर चढ़ते हुए
जिसे खर्चती हैं वे मोतियों की तरह
किसी धार2पर
ढलान में उतरते हुए या फिर चढ़ते हुए
इस तरह होती हैं उनकी अपनी जगहें
जंगलों के बीच भी
जहाँ वे जोर से हंसती हैं
जंगलों के बीच भी
जहाँ वे जोर से हंसती हैं
दरातियों के
नोक से ज़मीन को कुरेदते हुए
बहुत सारा नमक बो आती हैं
वे पहाड़ों पर
नोक से ज़मीन को कुरेदते हुए
बहुत सारा नमक बो आती हैं
वे पहाड़ों पर
२-
उगता है उनका नमक
अपनी ही बरसातों में
अपने ही एकांत में
अपनी ही काया में
अपनी ही ठसक में
वे बैठ जाती हैं तब
किसी धार की नोक में
टिके पत्थर पर
छमछट दीखता है
जहाँ से नदी का किनारा
दूर घाटी में पसरती नदी की तरह महसूस करती हैं
तब वे खुद को
उनके गादे3 से झांकती हैं
हरी पत्तियां बांज की
एकटक
अपने तनों से मुक्त
न्योली4गाते हुए
करती हैं वे संबोधित
अपनी ही भाषा में
अपने ही अनगढ़ शब्दों में पहाड़ को
अपनी ही भाषा में
अपने ही अनगढ़ शब्दों में पहाड़ को
वे गढ़ती हैं छीड़5
फिर गिरती हैं
और बुग्यालों में पसर जाती हैं
उनकी दराती तब
घास बनकर उगती है
चारों ओर हरी
घास बनकर उगती है
चारों ओर हरी
उनका यह महकदार नमक सीझता नहीं
बल्कि बिखर जाता है
वे फिर से काट लाती हैं
हरापन अपने घरों के भीतर
और बो आती हैं नमक फिर से पहाड़ों पर
बल्कि बिखर जाता है
वे फिर से काट लाती हैं
हरापन अपने घरों के भीतर
और बो आती हैं नमक फिर से पहाड़ों पर
३-
नमक बोती हुयी औरतें
थकती नहीं
याकि उन्हें थकना बताया ही नहीं गया है
थकती नहीं
याकि उन्हें थकना बताया ही नहीं गया है
वे होती हैं
एक शिकारी चिड़िया की तरह
जो खदेड़ देती हैं
बहुत दूर
एक शिकारी चिड़िया की तरह
जो खदेड़ देती हैं
बहुत दूर
अंगुलीवाले चीलों को
अपने घोंसले से
अपने घोंसले से
४ -
उनकी रातें भी होती हैं
अपने परदेस गये पतियों के लिए नहीं
अपने परदेस गये पतियों के लिए नहीं
बल्कि अपने दुखों को साझा करने
वे रातों को चल पड़तीहैं
मीलों दूर
जत्थों में
चांचरी6गाने
वे रातों को चल पड़तीहैं
मीलों दूर
जत्थों में
चांचरी6गाने
वे बहुत शातिर
छापामारों की तरह
कर देती है तब
रात को गोल घेरे में बंद
छापामारों की तरह
कर देती है तब
रात को गोल घेरे में बंद
वे हाथों में हाथ लेकर
बना लेतीं हैं चक्रव्यूह
जहाँ नहीं घुस पाती
उदासी
बना लेतीं हैं चक्रव्यूह
जहाँ नहीं घुस पाती
उदासी
तब फाटक पर टंगी
बोतलबत्ती
धधकतीहै
बांज के गिल्ठे
लाल हो रहे होते हैं कहीं किसी कोने में
उनके गीतों की हवा पाकर
बोतलबत्ती
धधकतीहै
बांज के गिल्ठे
लाल हो रहे होते हैं कहीं किसी कोने में
उनके गीतों की हवा पाकर
तब धूल उठती है
ज़मीन निखर जाती है
ज़मीन निखर जाती है
वह अपने पतियों के बिना भी रहती हैं खुश
पति उनके लिए केवल
होते हैं पति
या फिर फौजी कैंटिन के सस्ते सामान की तरह
पति उनके लिए केवल
होते हैं पति
या फिर फौजी कैंटिन के सस्ते सामान की तरह
५ -
पहाड़ पर नमक बोती औरतें
अपने परदेस जाते
पतियों को पहुँचाने
धार तक आती हैं हमेशा
अपने परदेस जाते
पतियों को पहुँचाने
धार तक आती हैं हमेशा
फिर लौट जाती हैं धार के उस तरफ
घास से भरे ढोके7लेकर
या पानी की गगरी कांख में दबाये
घास से भरे ढोके7लेकर
या पानी की गगरी कांख में दबाये
क्योंकि वे जानती हैं
लौट आते हैं परदेस गये लोग
अपनी ज़मीनों को एक दिन
लौट आते हैं परदेस गये लोग
अपनी ज़मीनों को एक दिन
इसलिए वे बसंत का स्वागत करती हैं
दरवाजों पर फूल
रखती हैं
बसंतपंचमी को
दरवाजों पर फूल
रखती हैं
बसंतपंचमी को
वे जाती हैं जंगल
दे देती हैं वह अपनी सारी टीस
हिलांस8को
दे देती हैं वह अपनी सारी टीस
हिलांस8को
अपने विरह को भूल जाती हैं
घुघूती9की सांखी10से निकलती घूर-घूर की आवाज में
घुघूती9की सांखी10से निकलती घूर-घूर की आवाज में
अपने रंग में रंग देती हैं जंगलों को
तब बुरांश11खिलता है लाल
काफल12में भर जाता है रस
तब बुरांश11खिलता है लाल
काफल12में भर जाता है रस
पहाड़ पर नमक बोती औरतें
महकदार नमक लिए
चलती हैं हमेशा
महकदार नमक लिए
चलती हैं हमेशा
६ -
पहाड़ पर नमक बोती औरतों
के होते हैं प्रेमी
वे खुद होती हैं महान प्रेमिकाएं
के होते हैं प्रेमी
वे खुद होती हैं महान प्रेमिकाएं
अपने देशाटन गये
पतियों से वे करती आई हैं
विद्रोह
और घुमक्कड़ों के साथ भागने के
उनके किस्से अब तक
जिन्दा हैं पहाड़ों पर*
पतियों से वे करती आई हैं
विद्रोह
और घुमक्कड़ों के साथ भागने के
उनके किस्से अब तक
जिन्दा हैं पहाड़ों पर*
वे भेड़ों का
रेवड़ लेकर
चली आती हैं भोट से
रेवड़ लेकर
चली आती हैं भोट से
कत्युर राजाओं के दरबारों तक
अपने प्रेम को व्यक्त करने
अपने प्रेम को व्यक्त करने
राजाओं के दरबारों से सुरक्षित
निकल भी जाती हैं
अपने जंगलों को
निकल भी जाती हैं
अपने जंगलों को
उन्हें पाने के लिए
राजा खोते आये हैं
अपनी सेनाएँ
राजा खोते आये हैं
अपनी सेनाएँ
अपनी ओर उठती जमींदारों की आँखें फोड़कर
भाग आती हैं वे अपने प्रेमियों के पास अक्सर
वे खोंच देती हैं बागनाथ की मूर्ति की आँखें
भगवानों के घूरने की आदत से परेशान होकर**
भगवानों के घूरने की आदत से परेशान होकर**
वे नदियों को देती हैं सोने के सिक्के दान***
कहती हैं बहती रहना
पत्थरों को मिट्टी बनाते रहना घिस-घिसकर
कहती हैं बहती रहना
पत्थरों को मिट्टी बनाते रहना घिस-घिसकर
तब जब वह बन जायेंगे मिट्टी
हम बो देंगीं उन पर नमक
७ -
पहाड़ पर नमक बोती औरतें
होती हैं माँएं
होती हैं माँएं
उनके बच्चे
खेलते हैं मिट्टी में
और खा भी लेते हैं
खेलते हैं मिट्टी में
और खा भी लेते हैं
मिट्टी का स्वाद जानते हैं
उनकी नाक बहती हैं
बहती हुयी नाक
का नमकीनपन
उन्होंने चखा है
उनकी नाक बहती हैं
बहती हुयी नाक
का नमकीनपन
उन्होंने चखा है
माँ के वक्ष से लगते हुए
यह प्रमाणित हो जाता है
खुद-ब-खुद
यह प्रमाणित हो जाता है
खुद-ब-खुद
पसीने से कुछ अलग नहीं होता
माँ के वक्ष का स्वाद
माँ के वक्ष का स्वाद
जो होठों पर चिपका रहता है
उनके जवान हो जाने पर भी
उनके जवान हो जाने पर भी
जवान होने से पहले वह
पहाड़ों पर खेलते हैं
फिसलनेवाला खेल
पहाड़ों पर खेलते हैं
फिसलनेवाला खेल
फिसलतेहुए
फट जाती है
उनकी पेंट पिछवाड़े से
और स्कूल की खाकी पेंट के पीछे हो जाते हैं छेद
जिन्हें वे आजीवन सीते रहते हैं फिर
माँओं से अलग होकर
फट जाती है
उनकी पेंट पिछवाड़े से
और स्कूल की खाकी पेंट के पीछे हो जाते हैं छेद
जिन्हें वे आजीवन सीते रहते हैं फिर
माँओं से अलग होकर
वह पहाड़ों पर
जाते हैं गाय चराने
तब रिभड़ाते हैं बैलों को
जाते हैं गाय चराने
तब रिभड़ाते हैं बैलों को
और जला देते हैं
सबसे ऊँचे पहाड़ पर खतडुवा13
उनकी माएँ
तब उनके लिए पकाती हैं
रोटी
और पीसती हैं नमक
सबसे ऊँचे पहाड़ पर खतडुवा13
उनकी माएँ
तब उनके लिए पकाती हैं
रोटी
और पीसती हैं नमक
८–
पहाड़ पर नमक बोती औरतें
जब कभी
पहाड़ों से
घास के ढोके के साथ
गिरती हैं
जब कभी
पहाड़ों से
घास के ढोके के साथ
गिरती हैं
छमछट ढलान पर
लुढ़कते हुए
नदी के पास पहुँच जाती हैं
या एक नदी हो जाती हैं
लुढ़कते हुए
नदी के पास पहुँच जाती हैं
या एक नदी हो जाती हैं
तब बदल दिया जाता है उस धार का नाम
उनकी शहादत पर
उनकी शहादत पर
पिताओं और पतियों के घर से
दूर इस जंगल में
में वे याद की जाती हैं हमेशा
घस्यारिनों द्वारा
में वे याद की जाती हैं हमेशा
घस्यारिनों द्वारा
तब शाम का पीला घाम केवल उनके लिए ही पसरता है पहाड़ों पर
ताकि सूख सके
मासिक धर्म में पहनी गयी उनकी धोती
ताकि सूख सके
मासिक धर्म में पहनी गयी उनकी धोती
इसी धूप में नहाती हैं वे गाड़-खोलों में
बैठ जाती हैं गाड़ के सबसे ऊँचे टीले पर
यही धूप मिलती है छुतियासैणी14को
सूरज की ओर से
पहाड़ लपक कर पकड़ लेता है इस धूप को
अपने सच्चे हक़दारों के लिए
यही धूप मिलती है छुतियासैणी14को
सूरज की ओर से
पहाड़ लपक कर पकड़ लेता है इस धूप को
अपने सच्चे हक़दारों के लिए
उस वक्त घरों पर बैठीं
पहाड़ पर नमक बोनेवाली औरतें
पहाड़ों से गिरी हुयी शहीद औरतों को
पहाड़ पर नमक बोनेवाली औरतें
पहाड़ों से गिरी हुयी शहीद औरतों को
याद करती हुयी
अपने बच्चों को बताती हैं
कि क्यों आता है पीला घाम पहाड़ों पर सांझ को ही
कैसे पड़ा होगा
नाम इस दुनिया में
जगहों का
पेड़ों का
चिड़ियों का
यहाँ तक की प्योली के फूल15का भी
पेड़ों का
चिड़ियों का
यहाँ तक की प्योली के फूल15का भी
और इस तरह बताती हैं
अपने इतिहास और अपनी लड़ाईयों में
वे राजधानी से दूर
किस तरह होती हैं शामिल
किस तरह होती हैं शहीद
किस तरह करती हैं गर्व
किस तरह उगती हैं ढलानों पर
किस तरह भींच लेती हैं ज़मीनों को अपनी जड़ों से
अपने इतिहास और अपनी लड़ाईयों में
वे राजधानी से दूर
किस तरह होती हैं शामिल
किस तरह होती हैं शहीद
किस तरह करती हैं गर्व
किस तरह उगती हैं ढलानों पर
किस तरह भींच लेती हैं ज़मीनों को अपनी जड़ों से
बच्चे सुनते हैं
और अधबीच में सुनते हुए सो जाते हैं
और एक लम्बे अन्तराल के बाद
अभिमन्यु घिर जाता है
चक्रव्यूह में
ज्यों ही जवान एकलव्य निकलता है
और अधबीच में सुनते हुए सो जाते हैं
और एक लम्बे अन्तराल के बाद
अभिमन्यु घिर जाता है
चक्रव्यूह में
ज्यों ही जवान एकलव्य निकलता है
अपने क़बीले से बाहर काट दिया जाता है
उसका अंगूठा
तब इतिहास में अर्जुन लिखे जाते हैं
गांडीव धनुष के साथ
गांडीव धनुष के साथ
जबकि पहाड़ पर नमक बोती औरतें
मरकर भी नहीं छोड़ती अपनी ज़मीनें
वे घट्ट16वालीगाड़
जंगलवाली धार
और नौले17वाले खोले18में रहती हैं मौजूद हमेशा
मरकर भी नहीं छोड़ती अपनी ज़मीनें
वे घट्ट16वालीगाड़
जंगलवाली धार
और नौले17वाले खोले18में रहती हैं मौजूद हमेशा
उनके हिस्से का नमक
उनके हिस्से का टीका
उनके हिस्से के कपड़े
उनके हिस्से की दरातियाँ
और उनके हिस्से का दर्पण आज भी
चढाता है जगरिया19
कहीं किसी धार पर डर के मारे
उनके हिस्से का टीका
उनके हिस्से के कपड़े
उनके हिस्से की दरातियाँ
और उनके हिस्से का दर्पण आज भी
चढाता है जगरिया19
कहीं किसी धार पर डर के मारे
मरकर भी नहीं छोडतीं वे
अपनी संगज्यों20को
हर दुःख में उन्हें देती हैं
लड़ने का हौसला
अपनी संगज्यों20को
हर दुःख में उन्हें देती हैं
लड़ने का हौसला
पहाड़ पर नमक बोते रहने की जिम्मेदारी से
कराती रहती हैं अवगत
कराती रहती हैं अवगत
वे सपनों में फटी धोती पहनकर चली आती हैं
मांगती हैं चूख
मांगती हैं नमक
महकदार
मांगती हैं चूख
मांगती हैं नमक
महकदार
बुलाती हैं जंगलों में
अपनी सहेलियों को
धार पर बैठकर सुनाने को कहती हैं न्योली
अपनी सहेलियों को
धार पर बैठकर सुनाने को कहती हैं न्योली
औरतें जाती हैं जंगल
और फिर-फिर बो आती हैं
नमक पहाड़ों पर
और फिर-फिर बो आती हैं
नमक पहाड़ों पर
***
1-चूख- बड़ा नीबू 2-धार - पहाड़ की चढाईयां, पर्वतों की चोटी 3- गादे- टांट के कपड़े से कमर में बाँध कर बनाया गया झोला 4-न्योली- एक विरहगीत जो गहन जंगलों के बीच घस्यारिनें गातीहैं 5 -छीड़-जलप्रपात या झरना 6- चांचरी- एक लोकनाट्यगीत - गोल घेरे में गाया जाता है 7- ढोके- रिंगाल की एक शंकुनुमा डलिया जो घस्यारिनें पीठ पर बांधती हैं 8- हिलांस -एक पहाड़ी पक्षी 9- घुघूती - पहाड़ों में विरह का प्रतीक फ़ाख्ता की प्रजाति का एक पक्षी 10 - सांखी-गर्दन 11- बुरांश -लाल रंग का एक पहाड़ी फूल 12- काफल - एक पहाड़ी रसीला जंगली फल 13 -खतडुवा- एक उत्सव जिसमें ऊँची पहाड़ी पर घास-फूस इकठ्ठा कर जलाया जाता है,मुख्यतः इसे जानवरों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है14 - छुतियासैणी- मासिकधर्म वाली स्त्री, पहाड़ों में इस दौरान इन्हें अछूत समझा जाता है और घर के सदस्य तक इन्हें नहीं छूते15- प्योंली-पीले रंग का एक फूल जिसके साथ लोककथाओं में किसी पहाड़ी स्त्री के पुनर्जन्म की कथा जुड़ी हुयी है16 - घट्ट- घराट 17-नौला- जलाशय 18- खोले - गधेरे 19- जगरिया -पहाड़ी ओझा, झाड़-फूंक करने वाला20- संगज्यों- साथी घस्यारिनें
*लोकश्रुतियों के अनुसार एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा को गया और उसकी पत्नी भानानाथ मत के प्रसिद्ध जोगी और घुमक्कड़ गंगनाथ के साथ भाग गई। गंगनाथ कुमाऊं में मूलतः दलितों का देवता माना जाता है।
**लोकगाथाओं के अनुसार कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रेमकथा राजुलामालुसाही की नायिका राजुलासौक्याण, भोट उसका क्षेत्र मध्यहिमालय में निवास करनेवाली रंजन जाति की बहादुर स्त्री जो कत्यूर राजा मालुसाही से प्रेम करती थी जिसने बागनाथ की मूर्ति की आँखें फोड़ डाली जो उसे घूर रही थीं और जमींदारों की भी आँखें फोड़कर अपने मालुसाही राजा के भवन तक पहुँची और शक्तियों से उसने पूरे राज्य को गहरी नींद में सुला दिया और राजा भी उसकी शक्ति से नहीं बचा सोये हुए राजा के सिरहाने वह एकपत्र लिखकर गई" अगर तूने अपनी माँ के स्तनों का दूध पिया है तो मेरे भोट आकर मुझे ब्याह कर ला तब तू सच्चा राजा" और फिर सुरक्षित अपने घर भी लौट गई राजा ने उसके इलाके में चढाई की और उसकी पूरी सेना इस युद्ध में ख़त्म हो गई।
*** नदियों को सोने के सिक्के दान देने वाली रंजन जाति की एक महिला झसुलीदताल


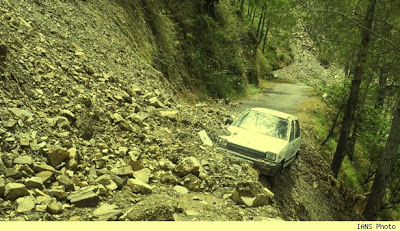


.jpg)






.jpg)










.jpg)



.jpg)
.jpg)






.jpg)
