आज साथी कवि तुषारधवल का जन्मदिन है और अनुनाद इस मौके पर उनकी चर्चित कविता काला राक्षस का पुनर्प्रकाशन कर रहा है। यह कविता इससे पहले सबद और अनुनाद पर ही छप चुकी है। तुषारधवल अपनी शुरूआत से ही जटिल वैचारिक किंतु नितान्त सामाजिक उलझनों के कवि रहे हैं और उनमें यही बात कहन की भिन्न दिशाओं के साथ अब भी मौजूद है। काला राक्षस पर हमारे अग्रज कवि वीरेन डंगवाल ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसे यहां लगाया जा रहा है। यह पोस्ट तुषार को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के साथ-साथ उनकी कविता पर बातचीत की शुरूआत के लिए भी है।
***
यह युवा कविता का मूल ऐजेंडे की तरफ़ लौटना है
"तुषार धवल की कविता 'काला राक्षस ' को पढ़ते हुए मुझे कई बार मुक्तिबोध-- खासकर उनकी 'अँधेरे में' की याद आई -- और कभी बंगला के समादृत समकालीन कवि नवारूढ़ भट्टाचार्य की प्रख्यात कविता 'यह मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश ' की. वैसी ही साफ़, वर्त्तमान से भविष्य तक को बेधने वाली दृष्टि, विवेक संपन्न चेतना, हर मोड़ पर मनुष्यता के शत्रुओं की पहचान, फुफकारता हुआ प्रतिरोध और आवेग त्वरित संवेदन सघन भाषा.मौजूदा तथाकथित वैश्वीकृत सभ्यता की समीक्षा करती हुई इस कविता में उत्कट बेचैनी, एक उद्विग्नता है जो सन्निपात के खतरनाक सीमांतों तक जा पहुँचती है. अलबत्ता लौट भी आती है उस तर्कशीलता के सहारे, जिसका दामन कवि ने एक पल को भी नहीं छोडा है. आवेग और संयम के इन आवर्तनों ने 'काला राक्षस' को एक ज़बरदस्त गत्यात्मकता दे दी है.'काला राक्षस' यह भी इशारा करती है कि युवतर हिंदी कविता का एक बड़ा और समर्थ तबका फिर अपने मूल एजेंडे की तरफ लौटने को प्रयत्नशील है. ठीक भी है. अपने ज़माने में मानवता की पुकारों को कलाएँ क्यों कर और कब तक अनसुनी कर सकती हैं ?"
-वीरेन डंगवाल
(१)
समुद्र एक
शून्य अंधकार सा पसरा है।
काले राक्षस के खुले जबड़ों से
झाग उगल-उचक आती है
दबे पाँव घेरता है काल
इस रात में काली पॉलीथिन में बंद आकाश
संशय की स्थितियों में सब हैं
वह चाँद भी
जो जा घुसा है काले राक्षस के मुंह में
काले राक्षस का
काला सम्मोहन
नीम बेहोशी में चल रहे हैं करोड़ों लोग
सम्मोहित मूर्छा में
एक जुलूस चला जा रहा है
किसी शून्य में
कहाँ है आदमी ?
असमय ही जिन्हें मार दिया गया
सड़कों पर
खेतों में
जगमगाती रोशनी के अंधेरों में
हवा में गोलबंद हो
हमारी ओर देखते हैं गर्दन घुमा कर
चिताओं ने समवेत स्वर में क्या कहा था ?
पीडाएं अपना लोक खुद रचती हैं
आस्थाएँ अपने हन्ता खुद चुनती हैं
अँधेरा अँधेरे को आकार देता है
घर्र घर्र घूमता है पहिया
(२)
काला राक्षस
वह खड़ा है जमीन से आकाश के उस पार तक
उसकी देह हवा में घुलती हुई
फेफड़ों में धंसती धूसर उसकी जीभ
नचाता है अंगुलियाँ आकाश की सुराख़ में
वह संसद में है मल्टीप्लेक्स मॉल में है
बोकारो मुंगेर में है
मेरे टीवी अखबार वोटिंग मशीन में है
वह मेरी भाषा
तुम्हारी आंखों में है
हमारे सहवास में घुलता काला सम्मोहन
काला सम्मोहन काला जादू
केमिकल धुआं उगलता नदी पीता जंगल उजाड़ता
वह खड़ा है जमीन से आकाश उस पार तक अंगुलियाँ नचाता
उसकी काली अंगुली से सबकी डोर बंधी है
देश सरकार विश्व संगठन
सत्ताओं को नचाता
उसका अट्टहास।
काली पालीथिन में बंद आकाश।
(३)
अट्टहास
फ़िर सन्नाटा।
सम्मोहित मूर्छा में
एक जुलूस चला जा रहा है
किसी शून्य में --
काल में
वह
हमारे मन की खोह में छुप कर बैठा है
जाने कब से
हमारे तलों से रोम छिद्रों से
हमरे डीएनए से उगता है
काला राक्षस
हुंकारता हुआ
नाजी सोवियत व्हाइट हाउस माइक्रोसॉफ्ट पेप्सी दलाल स्ट्रीट
सियाचीन जनपथ आईएसआई ओजोन एसपीएम एसिड रेन
स्किटज़ोफ्रेनिया सुइसाइड रेप क्राइम सनसनी न्यूज़ चैनल
बम विस्फोट !!!
तमाशा तमाशबीन ध्वंस
मानव मानव मानव
गोश्त गोश्त गोश्त
घर्र घर्र घूमता है पहिया
(४)
घर्र घर्र घूमता है पहिया
गुबार
उठ रही है अंधकार में
पीली-आसमानी
उठ रही है पीड़ा-आस्था भी
गड्डमड्ड आवाजों के बुलबुलों में
फटता फूटता फोड़ा
काल की देह पर
अँधेरा है
और काले सम्मोहन में मूर्छित विश्व
फिर एक फूँक में
सब व्यापार ...
देह जीवन प्यार
आक्रामक हिंसक
जंगलों में चौपालों में
शहर में बाज़ारों में
मेरी सांसों में
लिप्सित भोग का
काला राक्षस
(५)
एक छाया सा चलता है मेरे साथ
धीरे धीरे और सघन फिर वाचाल
बुदबुदाता है कान में
हड़प कर मेरी देह
जीवित सच सा
प्रति सृष्टि कर मुझे
निकल जाता है
अब मैं अपनी छाया हूँ। वह नहीं जो था।
पुकारता भटकता हूँ
मुझे कोई नहीं पहचानता
मैं किसी को नज़र नहीं आता
उसके हाथों में जादू है
जिसे भी छूता है बदल देता है
बना रहा है प्रति मानव
सबके साथ छाया सा चला है वह
अब कोई किसी को नहीं पहचानता
अब कोई किसी को नज़र नहीं आता
प्रति मानव !
कोई किसी को नज़र नहीं आता
(६)
तुमने काली अँगुलियों से गिरह खोल दी
काली रातों में
इच्छाएं अनंत असंतोष हिंसक
कहाँ है आदमी ?
उत्तेजित शोर यह
छूट छिटक कर उड़ी इच्छाओं का
गाता है
हारी हुई नस्लों के पराभूत विजय गीत
खारिज है कवि की आवाज़
यातना की आदमखोर रातों में
एक गीत की उम्मीद लिए फिर भी खड़ा हूँ
ढेव गिनता
पूरब को ताकता
तुमने काली अँगुलियों से गिरह खोल दी
काली रातों में
खोल दिया सदियों से जकड़े
मेरे पशु को उन्मुक्त भोग की लम्बी रातों की हिंसा में
(७)
बिकता है बिकता है बिकता है
ले लो ले लो ले लो
सस्ता सुंदर और टिकाऊ ईश्वर
जीन डीएनए डिज़ाइनर कलेक्शन से पीढियां ले लो
ले लो ले लो ले लो
बीपीओ में भुस्स रातें
स्कर्ट्स पैंटीज़ कॉन्डोम सब नया है
नशे पर नशा फ्री
सोचना मना है क्योंकि
हमने सब सोच डाला है
ले लो ले लो ले लो
स्मृतियाँ लोक कथाएँ पुराना माल
बदलो नए हैपनिंग इवेंट्स से
तुम्हारी कथाओं को री-सायकल करके लाएंगे
नए हीरो आल्हा-ऊदल नए माइक्रोचिप से भरेंगे
मेड टू आर्डर नया इंसान
ले लो ले लो ले लो
मेरे अदंर बाहर बेचता खरीदता उजाड़ता है
काला राक्षस
प्यास
और प्यास
(८)
इस धमन भट्ठी में
एक सन्नाटे से दूसरे में दाखिल होता हुआ
बुझाता हूँ
देह
अजनबी रातों में परदे का चलन
नोंचता हूँ
गंध के बदन को
यातना की आदमखोर रातों में
लिपटता हूँ तुम्हारी देह से
नाखून से गडा कर तुम्हारे
मांस पर
लिखता हूँ
प्यास
और प्यास...
एड़ियों के बोझ सर पर
और मन दस फाड़
खून पसीना मॉल वीर्य सन रहे हैं
मिट्टी से उग रहे ताबूत
ठौर नहीं छांह नहीं
बस मांगता हूँ
प्यास
और प्यास...
(९)
प्यास
यह अंतहीन सड़कों का अंतर्जाल
खुले पशु के नथुने फड़कते हैं
यह वो जंगल नहीं जिसे हमारे पूर्वज जानते थे
अराजक भोग का दर्शनशास्त्र
और जनश्रुतियों में सब कुछ
एक पर एक फ्री
हँसता है प्यारा गड़रिया
नए पशुओं को हांकता हुआ
(१०)
तुमने काली अँगुलियों से गिरह खोल दी
काली रातों में
निर्बंध पशु मैं भोग का
नाखून से गडा कर तुम्हारी देह पर
लिखता हूँ
प्यास
और प्यास...
भोग का अतृप्त पशु
हिंसक ही होगा
बुद्धि के छल से ओढ़ लेगा विचार
बकेगा आस्था
और अपने तेज पंजे धंसा इस
दिमाग की गुद्दियों में --
रक्त पीता नई आज़ादी का दर्शन !
लूट का षड़यंत्र
महीन हिंसा का
दुकानों की पर्चियों में, शिशुओं के खिलौनों में
धर्म और युद्ध की परिभाषा में भात-दाल प्रेम में
हवा में हर तरफ
तेल के कुएं से निकल कर नदी की तरफ बढ़ता हुआ
हवस का अश्वमेध
नर बलि से सिद्ध होता हुआ।
बम विस्फोट !!!
(११)
सबके बिस्तर बंधे हुए
सभी पेड़ जड़ से उखडे हुए
सड़क किनारे कहीं जाने को खड़े हैं
यह इंतज़ार ख़त्म नहीं होता
भीड़ यह इतनी बिखरी हुई कभी नहीं थी
काला सम्मोहन काला जादू
सत्ताओं को नचाता
उसका अट्टहास।
काली पॉलीथिन में बंद आकाश।
(१२)
वो जो नया ईश्वर है वह इतना निर्मम क्यों है ?
उसकी गीतों में हवास क्यों है ?
किस तेजाब से बना है उसका सिक्का ?
उसके हैं बम के कारखाने ढेर सारे
जिसे वह बच्चों की देह में लगाता है
वह जिन्नातों का मालिक है
वह हँसते चेहरों का नाश्ता करता है
हँसता है काला राक्षस मेरे ईश्वर पर
कल जिसे बनाया था
आज फिर बदल गया
उसकी शव यात्रा में लोग नहीं
सिर्फ़ झंडे निकलते हैं
(1३)
सत्ताएं रंगरेज़
वाद सिद्धांत पूँजी आतंक
सारे सियार नीले
उस किनारे अब उपेक्षित देखता है मोहनदास
और लौटने को है
उसके लौटते निशानों पर कुछ दूब सी उग आती है।
(१४)
पीड़ाओं का भूगोल अलग है
लोक अलग
जहाँ पिघल कर फिर मानव ही उगता है
लिए अपनी आस्था।
काला सम्मोहन --
चेर्नोबिल। भोपाल।
कालाहांडी। सोमालिया। विधर्व।
इराक। हिरोशिमा। गुजरात।
नर्मदा। टिहरी।
कितने खेत-किसान
अब पीड़ाओं के मानचित्र पर ये ग़लत पते हैं
पीड़ाओं का रंग भगवा
पीड़ाओं का रंग हरा
अपने अपने झंडे अपनी अपनी पीड़ा।
(१५)
कहाँ है आदमी ?
यह नरमुंडों का देश है
डार्विन की अगली सीढ़ी --
प्रति मानव
सबके चेहरे सपाट
चिंतन की क्षमताएं क्षीण
आखें सम्मोहित मूर्छा में तनी हुई
दौड़ते दौड़ते पैरों में खुर निकल आया है
कहाँ है आदमी ?
प्रति मानव !
(१६)
मैं स्तंभ स्तंभ गिरता हूँ
मैं खंड खंड उठता हूँ
ये दीवारें अदृश्य कारावासों की
आज़ादी ! आज़ादी !! आज़ादी !!!
बम विस्फोट !!!
कहाँ है आदमी ?
प्रति मानव सब चले जा रहे किसी इशारे पर
सम्मोहित मूर्छा में
मैं पहचानता हूँ इन चेहरों को
मुझे याद है इनकी भाषा
मुझे याद है इनकी हँसी इनके माटी सने सपने
कहाँ है आदमी ?
सुनहरे बाइस्कोप में
सेंसेक्स की आत्मरति
सम्भोग के आंकड़े
आंकड़ों का सम्भोग
आंकडों की पीढ़ियों में
कहाँ है आदमी ?
सन्नाटे ध्वनियों के
ध्वनियाँ सन्नाटों की
गूंजती है खुले जबड़ों में
यह सन्नाटा हमारी अपनी ध्वनियों के नहीं होने का
बहरे इस समय में
बहरे इस समय में
मैं ध्वनियों के बीज रोप आया हूँ।
(१७)
तुमने काली अँगुलियों से गिरह खोल दी
काली रातों में
उगती है पीड़ा
उगती है आस्था भी
जुड़वां बहनों सी
तुम्हारे चाहे बगैर भी
घर्र घर्र घूमता है पहिया
कितना भी कुछ कर लो
आकांक्षाओं में बचा हुआ रह ही जाता है
आदमी।
उसी की आँखों में मैंने देखा है सपना।
तुम्हारी प्रति सृष्टि को रोक रही आस्था
साँसों की
हमने भी जीवन के बेताल पाल रखे हैं
काले राक्षस
सब बदला ज़रूर है
तुम्हारे नक्शे से लेकिन हम फितरतन भटक ही जाते हैं
तुम्हारी सोच में हमने मिला दिया
अपना अपना डार्विन
हमने थोड़ा सुकरात थोड़ा बुद्ध थोड़ा मार्क्स फ्रायड न्यूटन आइन्स्टीन
और ढेर सारा मोहनदास बचा रखा था
तुम्हारी आँखों से चूक गया सब
जीवन का नया दर्शनशास्त्र
तुम नहीं
मेरी पीढियां तय करेंगी
अपनी नज़र से
यह द्वंद्व ध्वंस और सृजन का।
(१८)
काले राक्षस
देखो तुम्हारे मुंह पर जो मक्खियों से भिनभिनाते हैं
हमारे सपने हैं
वो जो पिटा हुआ आदमी अभी गिरा पड़ा है
वही खडा होकर पुकारेगा बिखरी हुई भीड़ को
आस्था के जंगल उजड़ते नहीं हैं
काले राक्षस
देखो तुमने बम फोड़ा और
लाश तौलने बैठ गए तुम
कबाड़ी !
जहाँ जहाँ तुम मारते हो हमें
हम वहीं वहीं फिर उग आते हैं
देखो
मौत का तांडव कैसे थम जाता है
जब छटपटाए हाथों को
हाथ पुकार लेते हैं
तुम्हारे बावजूद
कहीं न कहीं है एक आदमी
जो ढूंढ ही लेता है आदमी !
काले राक्षस !
घर्र घर्र घूमता है पहिया
****




.jpg)
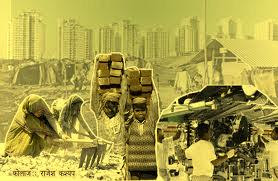.jpg)
.jpg)












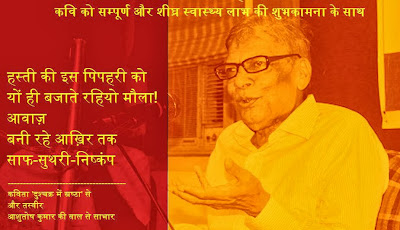.jpg)




.jpg)












.jpg)
