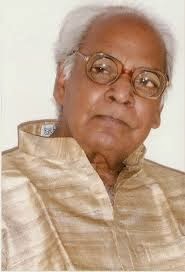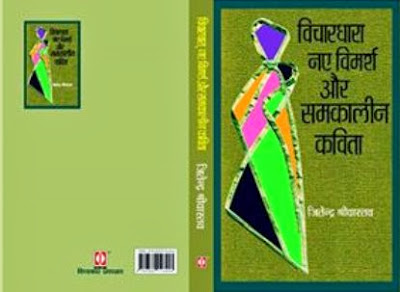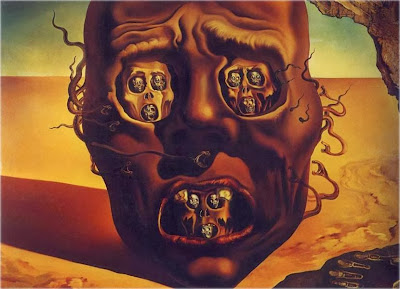इस वर्ष का सूत्र सम्मान सौरभ राय को दिया गया। उनकी कविताएं पाठक पहले अनुनाद पर पढ़ चुके हैं। अनुनाद कवि को सम्मानित होने की बधाई देता है और उनसे सम्मान के साथ मिली जिम्मेदारी को पूरी वैचारिक प्रखरता से निभाने की उम्मीद भी रखता है।
समारोह का संक्षिप्त विवरण
28 दिसंबर 2013 को बस्तर प्रान्त के जगदलपुर शहर में ठा. पूरन सिंह सूत्र सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस साल का सूत्र-सम्मान बैंगलोर के कवि सौरभ राय को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सौरभ राय के माता पिता भी उपस्थित थे, जो झारखण्ड से आये थे।
इस साल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि डॉ. प्रेमशंकर रघुवंशी थे, और कार्यक्रम की अध्यक्षता जोधपुर के चर्चित आलोचक एवं 'कृति ओर'के संपादक रमाकांत शर्मा ने की। सौरभ राय की कविताओं पर 'सर्वनाम'के संपादक रजत कृष्ण, और जगदलपुर के युवा आलोचक आशीष कुमार ने अपना अपना वक्तव्य पढ़ा। इसी परिसर में विभिन्न कवियों की काव्य रचनाओं पर कुंवर रविन्द्र के कविता-चित्रों की प्रदर्शनी भी लगी, जो बेहद चर्चित हुई। इस कार्यक्रम में जम्मू से आये कवि अग्निशेखर और बाँदा से आये केशव तिवारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय ग़ज़लकार राउफ परवेज़, वरिष्ठ कवि नरेंद्र श्रीवास्तव, मांझी अनंत, विकास यादव, त्रिजुगी कौशिक, निर्मल आनंद, नसीर अहमद सिकंदर, घनश्याम शर्मा सहित कई कवि एवं गणमान्य उपस्थित थे।
इसी अवसर पर जगदलपुर के जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ भी उपस्थित थे, जिनकी देख-रेख में कारागार के कैदी भाइयों ने मिलकर दो काव्य-संग्रहों एवं एक पत्रिका का प्रकाशन किया। कार्यक्रम में विशाखापट्टनम के कवि संतोष अलेक्स की कविता संग्रह 'पाँव तले की मिट्टी' और धमतरी के कवि युगल गजेन्द्र के काव्य-संग्रह 'वे कभी विरोध नहीं करते'का विमोचन, एवं विजय सिंह द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण पत्रिका 'समकालीन सूत्र'के नये अंक का लोकार्पण हुआ, जिसकी छपाई से लेकर जिल्दबन्दी का काम कैदियों ने ही किया। अगले दिन जेल के प्रांगण में तमाम कैदियों के बीच जगदलपुर आये कवियों ने काव्य पाठ किया। जेल के अँधेरे में जी रहे कैदियों के जीवन में साहित्य एवं काव्य की रोशनी भरने का यह एक ऐतिहासिक प्रयास था।
वक्तव्य और नई कविताएं
मैंने कोई वक्तव्य तैयार नहीं किया है। न ही यह सोच कर आया था कि कोई बड़ी बात करूँगा। वरिष्ठों से लेकर अग्रज कविगण, आज हम सब एक जगह पर उपस्थित हैं, जो स्वतः इस बात का प्रमाण है कि हमारे विचार मिलते हैं। हम कहीं भी हो सकते थे इस समय। कोई शौपिंग कर रहा होता, कोई प्रचलित फ़िल्म देख रहा होता, लेकिन हम देश के अलग अलग कोने से आकर बस्तर में एकत्र हुए हैं, यह प्रमाण है कि हमारे विचार मिलते हैं। पूरी तरह नहीं तो 80-90 प्रतिशत तो मिलते ही हैं। और जो 10 प्रतिशत विघटन है, यही तो है हमारी कविता, हमारी अलग अलग सोच का रहस्य! अगर हमारी समूची सोच एक जैसी हो जाए तो हमारी बातें और कवितायेँ भी एक जैसी हो जाएँगी। मेरे लिए कविता कुछ है, और आपके लिए कुछ और। ऐसे में अकादमिक बातें न कर के मैं कुछ अपनी बात करूँगा।
मैंने अपनी पहली कविता 8 साल के उम्र में लिखी, और वह थी - 'चेरापूंजी में सूखा पड़ा / एवेरेस्ट पर बाढ़ चढ़ा / काल नाचे ताता थैय्या / हंसिये मत / जब काटेंगे पेड़ तो ऐसा ही होगा भैय्या'बेहद साधारण सी कविता थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से ठीक-ठाक थी। पर मेरे परिवार के लोगों और शिक्षकों को इसमें कविता कम, सामान्य ज्ञान अधिक दिखलाई पड़ा। और देखते देखते मैं अपनी कक्षा का क्विज़ मास्टर बन गया। अपने सामान्य ज्ञान, विज्ञान के प्रति रुझान के कारण कई प्रतियोगिताएं जीतीं, स्कूल में, कॉलेज में अच्छे नंबर लाता रहा, और इंजीनियर बन गया। लेकिन इन सबके बीच कवितायेँ ज़िंदा रहीं। अंतर्मुखी था और काफी समय तक अपनी माँ और 4-5 मित्रों के बाहर मैं इन कविताओं को शेयर करने से भी बचता रहा। मुझे विदेशी फिल्मों का शौक था, जिन्हे मैं कॉलेज में रहते हुए डाउनलोड करके देखता था - अकीरा कुरोसावा, सत्यजीत राय, गोडार्ड इत्यादि की फिल्में। इन्ही से मैंने इमेजरी सीखी।
किताबें भी खूब पढ़ता था, लेकिन अंग्रेज़ी की ज्य़ादा। मार्क्स, गोर्की, मायकोव्स्की, कामू, सार्त्र से मुझे विचार मिले - ये सब ऑनलाइन पढ़ता था, अब खरीद कर पढ़ता हूँ। स्कूल कॉलेज में जो थोड़ा बहुत हाथ खर्च मिलता था, उससे कुछ प्रिय हिंदी कवियों की किताबें खरीदीं और इन्ही को बार-बार पढ़ते हुए मैंने डिक्शन पाया। इंजीनियरिंग के दूसरे साल तक मैंने लगभग 400 कविताएँ लिख दी थीं, लेकिन कोई भी कविता कहीं छपी नहीं थी, न ही मैंने इन्हे कहीं छपने के लिए भेजा था। इन्हीं दिनों मेरी सहपाठी और मित्र विद्या (जिससे मेरी अप्रैल, 2014 में शादी होने वाली है) ने सुझाया कि इनको संग्रह के रूप में आना चाहिए। बैंगलोर में रहते हुए, हिंदी के प्रकाशकों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन संकल्प इंडिया फाउंडेशन से जुड़े होने की वजह से डिजाइनिंग, छपाई, जिल्दबन्दी इत्यादि का काम जानता था। संकल्प एक संगठन है, जो कर्णाटक में रक्तदान को बढ़ावा देने को पिछले दस सालों से कार्यरत है। थैलेसेमिया से पीड़ित सरकारी अपस्ताल के 400 बच्चों को हम हर महीने समय पर निर्बाध और निशुल्क रक्त और दवाइयां देने का काम भी कर रहे हैं। संकल्प में मेरा एक काम पर्चे इत्यादि छपने का भी था, जिसकी वजह से संकल्प से जुड़े मेरे मित्रों और विद्या ने मिलकर मेरे पहले संग्रह -'अनभ्र रात्रि की अनुपमा'का प्रकाशन किया। इसके पैसे मेरे बाबा (पिता) ने दिए, जिनका प्रोत्साहन मुझे हमेशा मिलता रहा। यह एक स्वप्रकाशित संग्रह था जो वर्ष 2009 में आया। तब मैं इक्कीस साल का था।
इसके बाद मेरे दो और काव्य संग्रह 'उत्तिष्ठ भारत' 2011 में, और 'यायावर'दिसंबर 2012 में क्रमशः छपकर आये, जो स्वप्रकाशित थे। यायावर के छपने तक भी यह कवितायेँ किसी पत्र पत्रिका में नहीं छपी थीं। इन्ही दिनों मेरे एक मित्र ने कुछ कविताएँ हँस के सम्पादक राजेंद्र यादव जी को भेजीं, जिन्होंने इनको अपने जनवरी 2013 के अंक में स्थान दिया। इसी तरह फिर ये कवितायेँ 2013 में वागर्थ, वसुधा, कृति ओर, सर्वनाम, इत्यादि पत्रिकाओं; और पहली बार, अनुनाद जैसे ब्लॉगों में भी छपीं। कुछ प्रिय अग्रज एवं वरिष्ठ कवियों से बातचीत भी हुई, जिन्होंने प्रोत्साहित किया, और कंस्ट्रक्टीव सुझाव भी दिए। साहित्यकारों में एक अद्भुत समन्वय, एकजुट संघर्ष और आत्मीयता दिखलाई पड़ी। कुछ प्रिय कवियों के सुझाव से अपना उपनाम 'भगीरथ'भी हटा लिया। संग्रहों के संशोधित संस्करणों में, जहाँ से काफी कविताएँ निकाली जा रहीं हैं, यह बदलाव भी मुकम्मल होगा।
इन दिनों मैं पहले की तरह हड़बड़ाकर नहीं लिखता, और हर कविता को यथोचित समय भी देता हूँ। छपने का मोह शुरू से ही नहीं था, और अब कविताएँ पहले से अधिक फाड़ने भी लगा हूँ। कविता मेरे लिए एक संघर्ष रहा है, खुदको जानने, और अपने आसपास में होने, और जीवन को देखने समझने का साधन। और आप सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अगर इस सम्मान से जुड़ी अस्मिता और मानक की रक्षा कर पाया, तो यह मेरा सौभाग्य होगा।
***
होने में
बर्फ देख सोचता - इसकी नियति पानी
पानी देख नहीं लगा पाता अनुमान
बर्फ बादल या सागर ?
ईमारत देख शिकायत करता - ढह जाएगी
मलबा देख नहीं जान पाता घर कैसा रहा होगा ?
दीगर विषयों से मुश्किल इतिहास
कितनी रातें बीती ? सुबह कब होगी ?
समय में कहीं भी रहूँ, सोचता यही भोर !
मैं होने में समय तलाशता और होना मुझमें तलाशता समय
क्यों कैसे और कहाँ के पार
तलाशता 'कब'का जवाब
लकीर से कागज़, कागज़ से इंसान के बाद
तलाशता अस्तित्व का चौथा पहलू
सड़क पार करता सड़क की लम्बाई, मेरी चौड़ाई
सामने आती ट्रक की ऊंचाई जानने के बाद
पूछता ट्रक की गति, सड़क का इतिहास -
इसी सड़क से गुज़रे किसी राजा के रथ से नहीं टकरा पाया था मैं
और ट्रक मेरे समय में होकर भी रुका हुआ था
अपने पूरे वज़न से कोशिश की थी समय को रोकने की
और रुका हुआ था…
ट्रक के समय से गुज़रता हुआ कोशिश कर रहा था
रथ के समय से गुज़रने की
राजा के समय मेरा कौन था ?
मेरा कोई पुरखा
गुज़रा होगा जयकारे के बीच अपना होना तलाशता
राम के समय भी लड़ा होगा रावण के दल से
उसे शायद रामायण कंठस्थ ही न हो
- मेरे समय में होने का यह सबसे बड़ा प्रमाण था
आदिमकाल में जब पृथ्वी पानी था
अमीबा मैं; बाइनरी फिशन से बंटा होगा देशों की तरह
अलग अलग विलुप्त प्रजातियों से गुज़रता
मेरा होना जागा होगा किसी दिन ख़ुदको कीड़े में रूपांतरित देख
जंगल में कंद-मूल तलाशते - दौड़ना से देखना ज़रूरी
- सोच पहली बार खड़ा हुआ होगा दो पैरों पर
झिझककर हाथ मिलाने से इंकार करने की मुद्रा में फिर किया होगा
बहाना पीठ दर्द के इवोल्यूशन का
अपंग नवजात, हाथ की लकीरों पर हँसता
दुबक गया होगा अँधेरे में चार पैरों पर;
धारागत; फिर संगठित अंतःकरण के दलदल में खेत जोत
घर बना, धर्म बोल, देश के नाम पर कितनी बार
समय में अलग-अलग पक्ष से लड़ा मरा पैदा हुआ होगा
पुश्तों पीढ़ियों से लाखों प्रजातियों में
अनिश्चित समय पर निरुद्देश्य सम्भोग प्रजनन
जाती नस्ल के नियमों को जोड़ता तोड़ता
मेरा होना लगभग न होना
असंख्य शुक्रकणों में अनंतकाल से चयनक्रम का विलक्षण परिणाम
मेरा समय उसके समय में निराकार सा
जिसे देख चौंका होगा वह बार-बार
मेरा होना
लड़ रहा होगा लगातार मुझतक पहुँचने को
और पिघले बर्फ, ढही इमारतों से गुज़रकर
इस अस्तित्व तक पहुँचने की मेरी लड़ाई
मेरे होने में
शादी का फोटोग्राफर
उसकी लेन्स जिधर घूमती
ऊंघते लोग भी मुस्कुरा देते
मंत्र पढ़ता पंडित भी बोल उठता ज़ोर ज़ोर से
दूल्हा दुल्हन मौसा मौसी काका और बच्चे
चौकन्ने होकर करते कोशिश सामान्य दिखने की
कोई धीरे से फुसफुसाता - 'वो समय का वकील
बीते समय के प्रमाण जेब में लिए फिरता है'
थोड़ी देर बाद कौंधता कैमरा और
निर्वात में झांकते समय को एक फलैश में चीर
दर्ज़ कर लेता
लोग सोचते - मैं ज़यादा तो नहीं मुस्कुराया ?
आँखें बंद तो नहीं थी ?
भूत का डर
जन्म लेता यहीं से !
समय से नाख़ुश
वो हर नयी तस्वीर देख बड़बड़ाता
कर्वेचर एक्सपोज़र टीन्ट को गालियां देता
अलग अलग कोण से किसी की गरदन दायें
बच्चों को शांत औरतों को आगे
तीन सौ साथ डिग्री के विचार को पांच x सात इंच में समेटने का करता
बेहद महत्वपूर्ण काम
बिदाई के वक़्त भी अलग-थलग सा रहता
पिता के अँधेरे में तेज़ रोशनी
रोतीमाँ के झरते आंसुओं को लपक कर खुश होता
उन समयों को थाम लेता जो सदियों तक सबको हंसाती रहेंगी
वो जानता बेटी के जाने के बाद घर एक खाली नेगेटिव होता है
कैमरा रोता
और पूरे माहौल में मज़बूत उपस्थिति दर्ज़ करता सा
लगभग अनुपस्थित निराकार
नेपथ्य से झांकता
अचानक कहता -
स्माइल प्लीज़ !
छुट्टियों में घर
छुट्टियों में घर चला
अपने घर अपने बाबा के घर चला
उतना ही चला जितना घर मेरा था
साल में एक बार घर मेरा घर था
घर का एक कमरा कमरे का एक टेबल
उससे छिटकी रोशनी उससे दूर होता अँधेरा मेरा था
छुट्टियों में घर को फुर्सत थी मुझे अपनाने की
और मुझे थी फुर्सत अपना लिए जाने की
जिस घर में पैदा नहीं हुआ बड़ा नहीं हुआ
वह घर मुझमें पैदा होने की
बड़े होने की पुरज़ोर कोशिश कर रहा था
घर से मेरे पसंद की खुशबू आ रही थी
(आज मेरे पसंद की सब्जी बनी होगी
की जायेगी मेरे पसंद की बातें
घर में अनधिकृत गाँव में नए कपड़े पहन
मैं बन जाऊंगा गाँव का राजा बाबू
छोटी छोटी चीज़ों में बड़े अर्थ ढूंढता मैं बड़ा
बच्चों से बतियाउंगा सबको पसंद आऊंगा)
घर के बाहर का रास्ता मेरी परछाई थी
शांत ठंडी काली टेढ़ी मेढ़ी सी
रास्ते में जगह जगह गड्ढे थे
अपने रोज़मर्रा के झमेलों में चिंतामग्न
कुछ से अनजान कुछ मैं भूल चूका था
मेरे गड्ढों में पानी नहीं कीचड़ था
अपनी परछाई पर चल
घर का दरवाज़ा खटखटाता सोच रहा था
किसी अनजान आदमी ने दरवाज़ा खोला तो क्या कहूँगा ?
मेरा घर मुझमे प्रवेश कर रहा था
मेरे हिस्से की कवयित्री
मेरे हिस्से की कवयित्री कई हिस्सों की स्त्री है
अन्य पुरुष से खुद को देखती
अधीर, जड़ इतनी बूढ़ी कि लगभग एक बच्ची
लोगों को और लोगों के पार देखती
सुनती शब्दों को और निःशब्दों को भी
बूढ़ों की किलकारियों से चिढ़ती
बच्चियों की ख़ामोशी में नाराज़
कविता के नीचे अपना नाम पढ़ सोचती यह तो पुरुष !
इतनी सादी कि लगभग घमंडी
खुदको गालियां देती
बारिश की शाम खिड़की के शीशे पर बहते पानी को
आंसू समझ कर रो पड़ती
दूसरों की तारीफ़ पर हंसती
बुदबुदाती, मन और शरीर की उसकी ग़ैर ज़िम्मेदार हँसी
अराजक अनुगामी निराकार हंसी;
वो पार्टियों में घबरायी हंसती
स्त्री की आँखों में झाँकती
विचारों के पिंजरे को आँखों से टटोल सोचती चेहरा दृष्टि कैसे बने ?
पुरुषों की बात काट ठिठकती गलत नस काटने के बिम्ब में
स्त्री को देखती, परिधान समेत
सोचती क्या है इसके पास जो मेरे पास नहीं
बोध और यथार्थ के बीच तलाशती वो सब जो कर सकती
अभी इसी वक़्त मौका मिले अगर
आदर्श के लिए खड़ी रह सकती
कोई गिराने की कोशिश करे अगर
कोई इमारत से गिरे तो बचा सकती
जलते हुए को जान पर खेल बुझा सकती
वह सब कर सकती जो पुरुष करने की बात करते
अलक्षित नायिका सोचती असाधारण जीवन सरल
साधारण जीवन में ढूंढती कई कई व्यवधान
खुद के जीवन में अनवांछित मेहमान
मेज़बान को इतनी बार धन्यवाद बोलती
कि रह जाती लगभग चुप्प
वो चाहती लिखना भयमुक्त पत्थर के पेड़ के नीचे बैठ
अनादतन चाहती आदतें
बेंच के ऊपर बैठ ऊपर परिस्थिति
रुकी हुई और बदलती तेज़ रहस्यमय और अनावरित
जहाँ शब्द भिनभिनाते लफंगों की तरह;
वो सोचती कविता चलने में
बगल गुज़रते एक ही बिम्ब को रोज़ देखती
एक ही पंक्ति से वो सब तराशती जो कविता नहीं
आखिर में बचता अवसान; हाथ 'कुछ नहीं';
कभी लिखती इसलिए कि काले सूरज से लिख सके सफ़ेद दीवार पर
कविता के नीचे बना सके दिल,लिख सके नाम
फिर रो पड़ती अचानक - मैं दोषी ! कविता का गर्भपात !
ढूंढने लगती वो एक पुरुष जहाँ नहीं पहचानी जा सकती
बगीचे में टहलते फ़कीर को शराबखाने ले जाती
बोतल के पार लकीर को झुर्रियां, अँधेरे को झोपड़ी देख
लिखती – ‘मैं गरीब नहीं; संसाधनों की कमी में
रोटी देख ललचती अकेली नागरिक’
जन्म लेती उसके गर्भ में एक और स्त्री
शिव में काली ब्रह्मा में सरस्वती
पिंजरे में घूमती लट्टू पुतलियां
थक लुढ़क जाती आँखों में वापस;
रात भर उसकी प्रसव पीड़ा सिसकती
खिड़की में रहने वाले कृत्रिम सूरज को
उसकी आँखों को, आवाज़, रातों और सपनों को
दूसरी तरफ की मज़बूत दीवार पर लिखती रात भर;
उसके दृश्य उतने ही बिम्ब
जितने उसके शब्द
हर रात वो आधी रात पर रंगती
स्त्रीत्व का
पुरुषार्थ
बुखार में गिरना
मैं हो रहा हूँ नगण्य में तल्लीन
रंग काले और लाल; रात के वन-वे ट्राफिक को
पीछे से देखता लगातार गिर रहा हूँ
सुलगते कोयले से अगिनत बिम्ब उठ रहे हैं
एक दूसरे के प्रतिबिम्ब में झांकते तलाश रहे हैं वे
यथार्थ का रहस्य
मैं पुरुष प्रतीक सागर के बीच लेटा हुआ
एक ठंडा सांप सूखे पत्ते सा नीचे सरसरा रहा है
और एक स्त्री धो रही है मेरे सिर पैर
सामान्यीकरण के दुराभाव में दिन गिन रहा
सोमवार को सोमवार पुरुष को पुरुष स्त्री को स्त्री बोल रहा हूँ
देख रहा हूँ धूल जमता ख़ुद पर
धुल खतरनाक इसी के नीचे दब गयी कई कई सभ्यताएँ
बुखार में मेरा मन उछल कर खुदको झाड़ रहा है
और शरीर धीरे धीरे बदल रहा है
किसी विलुप्त सभ्यता के धसकते पिरामिड में
पूर्ण भाटे सा गले से फिसलता
बुखार का स्वाद चिकन सूप
(हाँ मान्साहारी)
शाकाहारी को सिर्फ जानवरों के भले अंत की चिंता !
मुझे मौत की क्या परवाह ? जितना कवि उतना आदमी
जानवर खा बुखार मना रहा हूँ; कविता के पहले ड्राफ्ट की तरह अपठनीय
जल रहा है मस्तिष्क; रोशनी में
प्रवेश करने का सोच दीये के इर्द गिर्द फड़फड़ा रहा हूँ
मर चुका हूँ और घृणित उन सबसे -
टेबुल बिस्तर फर्श किताबें - जो ज़िंदा रहेंगे
अपने हिस्से की रोशनी में सुबह ठन्डे शाम तक गर्म
कपकपाता सोच रहा हूँ - ज़िंदा रहना सचमुच एक अमानवीय स्थिति है
मेरे जीवन के मुंह में धंसा पारा परिप्रेक्ष्य में गिर रहा है
गिर रहे हैं रंग रोशनी रक्तचाप
और गिर रहा हूँ बुखार में मैं ।
***


.jpg)
.jpg)






.jpg)





.jpg)
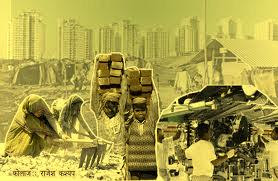.jpg)
.jpg)












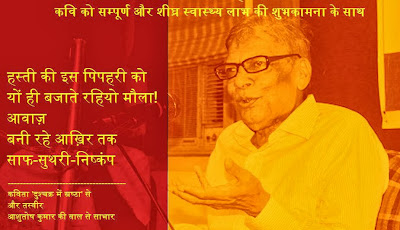.jpg)




.jpg)