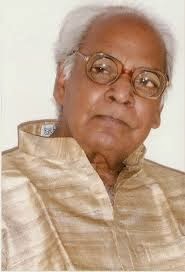It is midnight
I keep awake, all by myself
To see the midnight colors, they
Have silent is vibrant and
Rhythm eloquent- The midnight colors- Vijendra
अगर आप कविताओं मे रंग संयोजन, दृश्य-बिम्ब और तूलिकाओं के सघन स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं और चित्रकारी में कविता तलाश करना-चाहते हैं तो हमारी हिन्दी के एक विरल कवि हैं-विजेंद्र। ना सिर्फ़ कविता रचकर बल्कि कविता में जीकर,कविता के अंतःसौंदर्य को चित्रकारी में अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। लैटिन के महान कवि होरेस का वह कथन इनके संदर्भ में बिलकुल प्रासंगिक हो जाता है कि-‘’चित्र मूक कविता है’। इस संदर्भ में आलोचक जीवन सिंह का कहना है-‘’विजेंद्र स्वयं चित्रकला को कविता का पूरक मानते हैं।...चित्र कविता का पूरक इस अर्थ में भी है कि दोनों में सघन ऐंद्रिकता का बोध होता है।‘आधी रात के रंग’(The midnight colors)शीर्षक कविता की अंतिम पंक्तियाँ इसी सघन ऐंद्रिकता और विरल भावबोध का प्रमाण है-जिसमें कविता और कला का भेद-अभेद मिट जाता है।सौंदर्य गुलाबी हर्ष के साथ अवतरित हुआ है और मन कविता में लगा है।इस तरह अपने आप अपनी पेंटिंग पर कविता लिखने का या अपनी कविता पर पेंटिंग बनाने का अद्भुत काम इस कवि ने किया है-‘आधी रात के रंग’जैसे अनूठे संग्रह में। जहाँ कविता और कला एक दूसरे में संगुम्फित हो गयी है।
जबकि मैं महसूस करता हूँ
सुर्ख रंग की चीखें
आह्लाद भूरे रंग का
काले का भ्रूभंग
गुलाबी रंग का हर्ष ।
ये आधी रात के रंग
एक साथ मिलकर
नीरवता तोड़ते हैं
वे रात के ढुलकते बालों को
काढ़ रहे हैं।
अपनी पेंटिंग पर कविता टैगोर ने भी लिखी है और बाद में अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया है। इसी का विस्तार विजेंद्र के यहाँ हुआ है।जहाँ विजेंद्र ने कालिख से सनी रात में चित्रकारी का नायाब नमूना पेश किया है तो चाँद के उजास में कविता लिखने की हिम्मत का उदाहरण भी दिया है।हिन्दी और अँग्रेजी दोनों भाषाओं में एकसाथ यह काम अपने आप में ऐतिहासिक भी है,समीचीन भी,प्रासंगिक भी।
विजेंद्र जी के कवि-कर्म को अर्द्धशताब्दी पूरे होने को है।अपने लम्बे काव्य-जीवन में इन्होने बहुत कुछ लिखा है-वह भी प्रचुरता के साथ।सिर्फ़ कविता में नहीं बल्कि गद्य में भी-पर सबके केंद्र में या तो कविता है या कविता को लेकर गंभीर चिंतन!‘त्रास’से लेकर ‘बुझे स्तंभों की छाया’अर्थात 1966 से लेकर 2012 तक इनके कविता संग्रहों की प्रचुर दुनिया है।तेईस कविता-संग्रहों की भरी-पूरी दुनिया से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।कवितायें उत्कृष्ट हैं,मजबूत हैं,सुगठित हैं तो कवितायें साधारण भी,कमजोर भी,अनगढ़ भी हर तरह की कवितायें इनके यहाँ हैं।भले ही सारी रचनाएँ इनकी उत्कृष्ट नही हो,हालांकि किसी भी कवि की सारी रचनाएँ उत्कृष्ट नहीं होतीं चाहे महान से महान कवि ही क्यों ना हो?तो फिर विजेंद्र से इस तरह की उम्मीद लगाना भी उनकी रचनाशीलता के साथ खिलवाड़ करना है।इनके लेखन की भी अपनी सीमा है-जैसे कि सभी की।बात ये महत्वपूर्ण है कि इन्होने निरंतरता में सर्जना की है और बेहतर रचा है।
‘भीगे डैनों वाला गरुण’ 2010 में बोधि प्रकाशन से पुस्तक-पर्व योजना के तहत एक सेट में प्रकाशित हुआ संग्रह है।जिसकी कीमत मात्र दस रुपए है,और यह लगभग विजेंद्र की प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है।इसमें इनकी 1969 से लेकर 2009 तक की कवितायें हैं।इतने लम्बे समय की कविताओं में मुख्यतःइनकी लोकधर्मी चेतना,जीवनानुभावों की विविधता,जनसंघर्षों के प्रति आस्था,जीजीविषा,कविताई का स्थापत्य,संवेदना का सुसंगत और सुगठित रूप एक साथ देखने को मिल जाता है।इन कविताओं की दुनिया में सम्बन्धों का संयोजन है,जो एक खास तरह के मानवीय सरोकार के साथ जिनसे कविताओं में रचनात्मक शक्ति का विकास हुआ है।मनुष्यों के छल-छद्म,पाखंड और सम्बन्धों में धोखाधड़ी,काईंयापन से कवि हृदय का त्रस्त होना भी स्वाभाविक है।संवेदनहीन दुनिया से कवि को चिढ़ है-इसीलिए कवि जब आँख खोलकर दिल टटोलता है तो मन मसोसकर रह जाता है,फिर कविता लिखता है-
किसके पाँव पखारूँ भाया
किसकी करूँ मनौती
जिसको भी गले लगाऊँ
करता दिखे कनौती .......
विजेंद्र के अनुभवों की दुनिया भी एकदम विरल है,जिस अनुभव में सम्पूर्ण जीवन का यथार्थ अलग-अलग समय में अलग-अलग ढंग से प्रेषित होता है।अनुभवों के विस्तार से विजेंद्र कविता को भावों के उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं।वे सूक्ष्म-से सूक्ष्म वस्तुओं को कविता में ले आने की ताक़त रखते हैं। साथ ही गहरे मानवीय सरोकार और तरल भावावेग से युक्त ये कविताएं लोक के जीवन के सौंदर्य को रचने का दावा करती है। इन कविताओं की त्वरा और ताक़त सर्वथा भिन्न और देखने योग्य है।इसी संग्रह में एक कविता है-‘एक बच्चे के जन्म पर’।इस कविता में आवाज़ के माध्यम से कवि ने सम्पूर्ण ब्रह्मांड में एक बच्चे के जन्म के समय की आवाज़ को पूर्वजों और वंशजों के बीच से गुंजित कराते हैं।दरअसल में इसी आवाज़ का नाम परंपरा है,जिसे कवि पूर्वजों से ग्रहण कर वशजों को वितरित करना चाहता है।या यूं कहिए कि पूर्वजों से सुनी आवाज़ को वंशजों से सुन लेना ही यहाँ परंपरा-बोध है।यह कविता भावात्मक विस्तार की ऊचाइयाँ छूकर अनुभव जगत में प्रकृतिक अवयवों से संवाद कर एक भरी-पूरी अनोखी दुनिया में अनायास प्रवेश कर जाती है, जहाँ कविता और चित्र का भेद मिट जाता है।कुछ पंक्तियाँ देखिये-
ये पठारों की तरह कठोर, पतझर की तरह सूखी
और वर्षा की तरह गीली।
मैंने कई बार इन्हें अपने निजी प्यार की संज्ञा दी है
आदमी के मुक्त होने से पूर्व
सारा देश इन्हें हवाओं के साथ सुनता है........
इस एक कविता में कवि ने एक-एक पंक्ति में नए-नए अर्थबोधों को पिरोकर रख दिया है।पाठ में सुरुचि उत्पन्न करनेवाली यह कविता बिम्ब-सृष्टि में गज्झिन है।प्रत्येक पंक्ति में नए-नए प्रतीको को सँजोया गया है-उपमा की सहजता के साथ।‘उपमा कालीदासस्य’वाली शास्त्रीय उक्ति यहाँ चरितार्थ हो जाती है।
‘एक बच्चे के जन्म पर’कविता में ही कवि आगे कहता है-जिन आवाजों को वे सदियों से सुन रहे हैं वे समुद्र की तरह विशाल और मरुस्थल की तरह उतप्त हैं।कवि ने आवाज़ों के उद्गम-स्थल धरती के गर्व को माना है।इसीलिए पृथ्वी के जितने अवयव हैं सबसे कवि ने उस आवाज़ को चीन्हने में सहायता ली है।पठार,मरुथल,समुद्र,पतझर,वर्षा से लेकर हवाओं की तरह यानि सभी प्रकृतिक वस्तुओं से निःसृत आवाज़ है-वह।या सभी प्राकृतिक वस्तुएँ उस आवाज़ को(ध्वनि को)शक्ति देती है,ऊर्जा ग्रहण कराती है।ये बांक की तरह पैनी और फूलों की तरह नरम है,ठीक अगली पंक्ति में घने जंगल कटते समय जाड़े की अंधेरी रात में उस आवाज़ को सुनना-पूरी प्रकृति को बचाने की कवि की युक्ति नहीं तो और क्या है?
कवि की प्रतिबद्धता आगे गहरे अर्थों में मानवीय हो जाती है जब कवि बच्चों की हंसी,माँ के प्यार और दोस्त की सच्चाई की संज्ञा से उस प्यार को पहचानता है।हर बार लौह-शृखलाओं की आकृतियों का उभरना यहाँ पर साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ते सर्वहारा की संगठित शक्तियों का प्रतीक है।काँटेदार तारों के क्रूर बाड़े,धातुओं का चुपचाप पिघलना उसकी बेचैनी,जहरीले हथियारों से पड़े भद्दे निशान की तरह है वो आवाज़ जिसको कवि सुनता जाता है।एक आदमी का किसी और के लिए फसल काटकर अपना जिस्म सुखाने का अर्थ स्पष्ट है कि श्रम से पसीना किसी और का बहे और श्रम का लाभ कोई और ले जाये।आगे कवि लिखता है-‘’रात में खादर का किसान खेत में पानी काटता है/जब माँ बच्चों को दूध पिलाती है/जब मैं तुम्हारे सूखे बालों में गुड़हल का फूल खौंसता हूँ...’’यह उस सर्वहारा की आवाज़ के साथ अपना संतुलन बैठाकर आवाज़ों का संतुलन बनाना भी वैज्ञानिक साउंड थेओरी का विस्तार लगता है,जिसका वेवलेंथ कोंस्टेंट नहीं है।कवि अपनी आँखों से जंगल के उस मनुष्य को भी देख लेता है जो काले-काले नरकंकाल हैं ,जिसके घने बाल उसके जिस्म ढकने के काम आते हैं।कवि उस मनुष्य की बात करता है जो डार्विन की विकसवादी अवधारणा में कहीं बहुत पीछे छूट गया हाशिये का मनुष्य है,जिन्हे आदिवासी’की संज्ञा दे दी गयी है।उस आदिवासी समाज के पक्ष में कवि का खड़ा होना उन्हें वाजिब कवि तो बनाता ही है,साथ-ही-साथ उन्हें मुकम्मल मनुष्य भी बनाता है।एक बच्चे का जन्म कवि के लिए उस विराट का आगमन है जो सम्पूर्ण मनुष्यता,अखिल विश्व और पूरे ब्रह्मांड के कण-कण को प्रभावित करनेवाली भविष्योनमुखी स्वर का द्योतक है।
विजेंद्र की कविताओं की दुनिया इतनी विस्तृत है(और इतनी प्रचुरता में इनका लेखन है) जिसपर लिखना दुरूह कार्य तो है ही।पर जहां तक मेरी दृष्टि जा पायी है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि विजेंद्र हमेशा अनछूए विषयों को ही कविताओं में छूते हैं।सारी अनछूई वस्तुएँ इनकी कविताओं की विशेषता बन जाती है तो कहीं पर वह अर्थ के विपरीत अर्थों को भी ग्रहण कर लेती है।इससे कविताओं के अंदर कभी भावों सरलीकरण हो जाता है तो कहीं पर अर्थ दोष भी उत्पन्न हो जाता है।
इनके अंदर लोक की गहरी समझ और विश्व कविता का गंभीर अध्ययन दोनों है,जिससे इनकी कविताओं की रचना-प्रक्रिया मजबूत होती गयी है,शिल्प सुगठित होता गया है,भाषा निखरती गयी है। विजेंद्र के सौंदर्य दृष्टि की जितनी प्रशंसा की जाय कम है,सौंदर्यशास्त्र पर व्यवस्थित चिंतन भी इनहोने किया है।‘सौंदर्यशास्त्र भारतीय चित्त और कविता’शीर्षक पुस्तक इसी बात का प्रमाण है।इस पुस्तक के बहाने भी विजेंद्रजी ने सौंदर्यशास्त्र की अवधारणा का भारतीय चित्त और कविता के इसपर प्रभाव का बहुत सफलतापूर्वक रेखांकन किया है।इसमे सौंदर्य के दार्शनिक आधार से लेकर तुलसीदास को जातीय क्लैसिक की पहचान करनेवाले कवि के रूप में चिन्हित किया गया है।
विजेंद्र की कविताओं की बिम्ब सृष्टि में एक साथ सभी ज्ञानेद्रियाँ प्रभावित होती हैं कविताओं की बदौलत।प्रतीकों का उपयोग भी कवि ने एक सुशिक्षित कवि के रूप मे किया है।कविताओं में दृश्यात्मक्ता इतनी कि कविता और चित्रकारी एक दूसरे के पूरक हों।‘स्यानी चिड़िया’,’कठफोडवा’,’भीगे डैनों वाला गरुण’,’अगर मेरे पंख होते’ आदि कविताएँ कवि के पक्षी प्रेम को एक तरफ दर्शाती है तो निर्द्वंद्व और निर्भीक स्वर के प्रति कवि की प्रतिबद्धता को इंगित करती है।यहीं से जीवन और जगत के प्रति एकनिष्ठ जीवटता आती है।जहां छल,छद्म,पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है।निर्भ्रांत भावों से मुक्तिकामी स्वरों की पहचान करने में विजेंद्र सक्षम रहे हैं,तदनुरूप बिम्ब भी गढ़ लेते हैं,भाषा भी निर्मित कर लेते है।जहाँ जीवन और कविता एक-दूसरे में संगुंफित हो जाती है।
‘’अब ये मुझे लगा
पंख देह की शोभा नहीं
मेरा जीवन है ....’’
पंछी के बहाने कवि जीवन-सौंदर्य रचने का दावा लेकर मुक्ति की कामना करते हैं।वैसी कामना जिसकी गूंज पारंपरिक रूप से हिन्दी कविता में सुनाई देती रही है-‘लेकिन पंख दिये हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो.....’’कठफोडवा’ कविता की आखिरी पंक्ति देखिये-
मुझे लगा तू आज़ाद होकर भी
क़ैद है
इतने खुले वन में
कहीं-न-कहीं-क़ैद! क़ैद!
रेत के बड़े-बड़े निर्जन टीले पर उगने वाले फूल ‘मरगोजा’ पर भी कवि विजेंद्र ने कविता लिखी है।जिसका खिलना वसंत के आगमन की सूचना है।हर अनछूई वस्तुओं पर लिखी इनकी कविता हमे उस लोक में ले जाती है जहाँ से वस्तुएँ जीवन की अनिवार्यता का एहसास कराती है।
 विजेंद्र जी ने न सिर्फ लोकधर्मी चेतना से ओत-प्रोत कविताएँ लिखी है बल्कि लोकधर्म की समकालीनता की दुर्लभ व्याख्या भी इनहोने की है।जिसके बहाने कवि लोक-संवेदना का शास्त्र पाठक के सामने रखने में सक्षम हुआ है।इसीलिए ये कविता की रचना-प्रक्रिया के शास्त्र को रचने वाले विरल समकालीन रचनाकार हैं।इसीलिए समकालीन कविता पर होने वाली हर बहस में विजेंद्र का नाम आना अस्वाभाविक नहीं है।कारण है विजेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा और विस्तीर्ण काव्य-संवेदना के साथ-साथ विरल लोक-शिल्प।विजेंद्र की कवितायें रेगिस्तान के बंजारों के उस लोकगीत की तरह है जिसे जीवन गा रहा है।इनकी चित्रकारी उस आमूर्त अभिव्यक्ति में निर्मित कला का प्रमाण है,जिसमें मानव जीवन अपने हर स्वरूप में मौजूद है।इसीलिए इस अद्भुत शिल्पकार के पास भावों का ऐसा ऐंद्रिक स्पर्श है जिसके कोर-कोर में जीवन भी है और उसकी गतिशीलता भी.......
विजेंद्र जी ने न सिर्फ लोकधर्मी चेतना से ओत-प्रोत कविताएँ लिखी है बल्कि लोकधर्म की समकालीनता की दुर्लभ व्याख्या भी इनहोने की है।जिसके बहाने कवि लोक-संवेदना का शास्त्र पाठक के सामने रखने में सक्षम हुआ है।इसीलिए ये कविता की रचना-प्रक्रिया के शास्त्र को रचने वाले विरल समकालीन रचनाकार हैं।इसीलिए समकालीन कविता पर होने वाली हर बहस में विजेंद्र का नाम आना अस्वाभाविक नहीं है।कारण है विजेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा और विस्तीर्ण काव्य-संवेदना के साथ-साथ विरल लोक-शिल्प।विजेंद्र की कवितायें रेगिस्तान के बंजारों के उस लोकगीत की तरह है जिसे जीवन गा रहा है।इनकी चित्रकारी उस आमूर्त अभिव्यक्ति में निर्मित कला का प्रमाण है,जिसमें मानव जीवन अपने हर स्वरूप में मौजूद है।इसीलिए इस अद्भुत शिल्पकार के पास भावों का ऐसा ऐंद्रिक स्पर्श है जिसके कोर-कोर में जीवन भी है और उसकी गतिशीलता भी.......