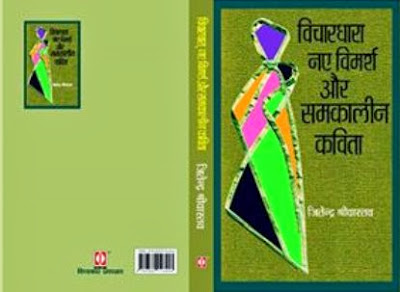आज की आलोचना विशेषकर व्यवहारिक आलोचना का एक बड़ा संकट है-उसे न पढ़े जाने का।विडंबना यह है कि इसका कारण इसके लिखे जाने में ही छुपा है। आज जिस प्रायोजित और चलताऊ(बिना पढ़े ही) ढंग से व्यवहारिक आलोचना लिखी जा रही है उसने इसकी गंभीरता और विश्वसनीयता को गहरा धक्का पहुँचाया है।जब पाठक को पता हो कि अमुक आलोचना किसी कवि विशेष को उठाने या गिराने के उद्देश्य से लिखी गई है तब भला वह उसको पढ़कर अपना समय खराब क्यों करे?ऐसे बहुत कम आलोचक हैं जो इस क्षेत्र में पूरी तैयारी और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं तथा अपने आलोचना धर्म का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं।उन बहुत कम आलोचकों में से एक नाम है- जितेन्द्र श्रीवास्तव। वह मूल रूप से एक कवि हैं लेकिन आलोचना के क्षेत्र में किए जा रहे लगातार हस्तक्षेप ने उन्हें एक गंभीर और ईमानदार आलोचक के रूप में पहचान दी है।आज वह कविता और आलोचना दोनों विधाओं में समान रूप से सक्रिय हैं। सद्य प्रकाशित ‘विचारधारा नए विमर्श और समकालीन कविता’ आलोचना की उनकी पाँचवी पुस्तक है। विषयवस्तु की दृष्टि से इस पुस्तक को मोटे रूप में पाँच हिस्सों में बाँटकर देखा जा सकता है। पहले हिस्से में ‘समकालीन हिंदी कविताःनई चुनौतियाँ’ व ‘समकालीन हिंदी कविता की भारतीयता’ विषयक आलेख ,दूसरे हिस्से में हिंदी की दलित कविता का मूल्यांकन, तीसरे हिस्से में स्त्री-दृष्टि और कविता ,चौथे हिस्से में वरिष्ठ पीढ़ी के कवियों तथा पाँचवे में नब्बे के दशक के बाद के कवियों की कविताओं का मूल्यांकन।
वह समकालीन हिंदी कविता की नई चुनौतियों से अपनी बात प्रारम्भ करते हैं। उनके अनुसार कविता के सामने पहली चुनौती उसका गद्यमय होते जाना है। इस संकट के लिए वह उन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं जो ‘‘कविता की मूल प्रकृति को दरकिनार करते हुए पाठकीय आकांक्षाओं को कालापानी देते हुए कुछ-कुछ कविता लिखते रहते हैं और उसे कविता कहते हैं।ये वे लोग हैं जो कविता की आदि ताकत ‘लोक’ और ‘लोकतत्व’ से घृणा करते हैं।’’ दूसरी चुनौती वह संप्रेषणीयता को मानते हैं जिसके चलते नब्बे के बाद पाठक और श्रोता कम हुए हैं।उनका यह प्रश्न तर्कसंगत है कि कविता के नाम पर अर्थहीन प्रयोग और लद्धड़ गद्य कोई क्यों पढ़ना चाहेगा? इनके अलावा ‘ग्रामीण जीवन के यथार्थ’ का कविता में न के बराबर आना,कविता को खेल समझने का प्रचलन बढ़ना,कविता के पास अपना मुक्कमल आलोचक न होना आदि उनके अनुसार कुछ अन्य चुनौतियां हैं।इन चुनौतियों और उनके कारणों पर अपने आलेख में जितेन्द्र ने विस्तार से चर्चा करते हुए इस निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि कविता कभी समाप्त नहीं होगी। आलोचक का यह विश्वास दरअसल मानव की संवेदनशीलता और अच्छाई पर विश्वास है।
लोकधर्मी कवि-आलोचक जितेन्द्र को अपनी जड़ों से गहरा लगाव है। वह जड़ों से जुड़े रहने का महत्व भी समझते हैं। इसलिए वह कविता में भारतीयता,स्थानीयता तथा लोकतत्व की पड़ताल करते हैं। उनका लोक और लोकतत्व को कविता की आदि ताकत मानना यूँ ही नहीं है। उनके लिए भारतीयता का मतलब भूमंडलीकरण की आंधी में अपने साहित्य की निजता का भावबोध है। वह कवियों को अनुभवों के अनुवाद और अनुवाद की भाषा से बचने की सलाह देते हैं। ऐसा वही आलोचक कह सकता है जिसको अपनी पहचान को बचाए रखने की अहमियत पता हो।उनका यह मानना सही है कि हिंदी कविता का मूल चरित्र ही भारतीय रहा है।उसके शब्द-शब्द से भारतीयता झांकती है। हिंदी में मानवीय संबंधों पर लिखी गई कविताओं का नजरिया ठेठ भारतीय है। जितेन्द्र अपनी इस मान्यता की पुष्टि में हिंदी कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कविताओं को सामने रखकर बात करना आलोचना की एक सही पद्धति है। अन्यथा आलोचना के अमूर्त होने खतरा रहता है। इस संदर्भ में वे त्रिलोचन,केदारनाथ सिंह, असद जैदी ,एकांत श्रीवास्तव, रघुवीर सहाय, अनामिका, राकेश रंजन,राजेश जोशी,बद्रीनारायण,अरुण कमल, देवी प्रसाद मिश्र,विष्णु खरे,मंगलेश डबराल,उदय प्रकाश, स्वप्निल श्रीवास्तव आदि कवियों की कविताओं का उद्धरण करते हैं। लेकिन वह यह कहना नहीं भूलते हैं कि स्थानीयता और विश्वबोध ही किसी रचना को वृहत्तर धरातल निर्मित करते हैं।
एक अच्छी बात यह है कि जितेन्द्र ने कवियों के साथ-साथ कवयित्रियों पर भी बराबर ध्यान दिया है। स्त्रियों द्वारा लिखी जा रही और स्त्रियों पर लिखी गई दोनों कविताएं उनके नजरों से ओझल नहीं होती हैं। उनका मानना है कि युवा कवियों में स्त्री जीवन के प्रति पूरी संवेदनशीलता और प्रगतिशीलता दिखाई देती है। इस पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा स्त्री विमर्श पर है। आलोचक किसी भी कवि की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए उसकी स्त्री विषयक कविताओं को रेखांकित करना नहीं भूलता। इस पुस्तक में ‘स्त्री दृष्टि और कविता’पर तीन आलेख हैं जिनमें वर्तमान में हिन्दी कविता में जिन कवयित्रियों की प्राणवान उपस्थिति है उन सभी की कविताओं का सम्यक विश्लेषण है। एक आलेख में रघुवीर सहाय की स्त्रियों से संबंधित कविताओं में स्त्री-जीवन की विडंबनाओं और स्त्रियों के संघर्ष की पड़ताल की गई है। इन आलेखों की खासियत है कि इनमें केवल कविता पर बात न होकर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की दशा,उसमें आ रहे परिवर्तन और उसके संघर्ष पर भी बात हुई है। इससे स्त्रियों के प्रति आलोचक के दृष्टिकोण का पता भी चलता है। अच्छी बात यह है कि इन आलेखों में आलोचक न केवल स्त्री जीवन की त्रासदी बल्कि इस त्रासदी से मुक्ति का रास्ता भी बताता चलता है। उसका दृढ़ विश्वास है कि स्त्री स्वाधीनता तभी पूर्ण होगी जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंत होगा। जब वह इस सामंती ढाँचे से मुक्त होगी। लेकिन वह इस बात से भी भली-भांति परिचित हैं कि बहुत संभव है कि स्त्रियां सामंती ढाँचे से मुक्ति की आकांक्षा में पूँजीवादी जाल में फंस जाएं। इसलिए जरूरी है कि वे इस पड़ाव को भी लांघें-अपनी सचमुच की आजादी के लिए।
स्त्री विमर्श की तरह दलित विमर्श को भी प्रस्तुत पुस्तक में पर्याप्त स्थान मिला है। दलित जीवन से जुड़े कवि हीरा डोम से लेकर नई पीढ़ी में रचनारत दलित कवियों की चर्चा यहाँ हुई है। इसमें जितेन्द्र नए सौदर्यशास्त्र का प्रश्न उठाते हैं और उसके गढ़े जाने का कारण बताते हैं। उनका मानना है कि हिंदी का दलित साहित्य महानता के स्याह अंधेरे के विरूद्ध उजाले का संदेहवाहक है। उनका यह विश्लेषण बिल्कुल सही है कि ‘‘ पूरा का पूरा दलित साहित्य ‘वर्ण विद्रोह’ का साहित्य है। यही वजह है कि शोषितों-वंचितों के पक्ष में खड़ा मार्क्सवादी सौंदर्यशास्त्र भी‘दलित साहित्य’ को समझने एवं समझाने में पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाया है।’’ उनकी इस बात से मेरी भी पूरी सहमति है कि दलित साहित्य के विश्लेषण में ‘वर्ग’ की समझ से अधिक ‘भारतीय जाति व्यवस्था’ और उसकी ‘क्रूरता’ की समझ आवश्यक है।’’ वह दलित साहित्य की उपयोगिता को कुछ इस तरह रेखांकित करते हैं कि एक ‘दलित सर्वहारा’ की पूर्ण मुक्ति तभी संभव होगी जब सामाजिक और मनोगत संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन होगा.....दलित साहित्य इस परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहा है और उसका सौंदर्यशास्त्र इसी संघर्ष की कोख से पैदा हुआ है।’’ इस तरह दलित साहित्य की पड़ताल के उनके अपने औजार हैं। बहुत सारे आलोचकों का आरोप है कि दलित कविता में कला का अभाव है। उसमें कवि के कच्चे अनुभव अनुभूति में नहीं बदल पाए हैं बल्कि कोरे अनुभव अधिक व्यक्त हुए हैं। लेकिन जितेन्द्र इससे भिन्न मत रखते हैं-कला कम हो लेकिन जीवन खूब हो तो कविता बन जाती है।वह एक ऐसी कविता होती है जिसके निश्चित सामाजिक निहितार्थ होते हैं। वह मनुष्य की सहचर बनती है। उनकी यह मान्यता इस बात का प्रमाण है कि जितेन्द्र साहित्य चिंता की अपेक्षा जीवन चिंता के आलोचक हैं।उनकी आलोचन में जीवन से निकटता और यथार्थ से लगाव दिखाई देता है। वह जीवन के सवालों से मुटभेड़ करते हैं। उनका जीवन से जुड़ाव ही है जो उन्हें लोक और जनपद प्रेमी बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं मान लिया जाय कि जितेन्द्र कविता में कलात्मकता की उपेक्षा करते हैं। वह इस बारे में बिल्कुल साफ हैं,‘‘सही अर्थों में कवि कहलाने का हक उसी को है जो वैचारिकता और कलात्मकता के रसायन को बूझता-समझता हो और यह जानता हो कि किस कविता में कितनी कला और कितना विचार होना चाहिए।’’ वह कविता में कला,जीवन और विचारों की अविच्छिन्न संगत की माँग करते हैं।
युवा आलोचक जितेन्द्र श्रीवास्तव की कोशिश है कि श्रेष्ठ सृजनात्मकता को रेखांकित किया जाय और ‘कविता में चित्रित घनघोर निराशा के गर्भगृह में बैठी आशा की पहचान’ कराई जाए। यह पुस्तक उसी दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह किताब इस अर्थ में अलग है कि इसमें वरिष्ठ ही नहीं कनिष्ठ से भी कनिष्ठ पीढ़ी के उन कवियों को भी इसमें शामिल किया गया है जिन्होंने 21वीं सदी के पहले दशक में लिखना प्रारम्भ किया। इसमें एक ओर जहाँ वरिष्ठ पीढ़ी के कवियों की ताकत की तो दूसरी ओर नई पीढ़ी की संभावनाओं की जाँच पड़ताल की गई है। आलोचक का सकारात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान गया है। यह काम आग्रहों व पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर किया गया है। वह कविता के पास पूरी सजगता किंतु विनम्रता के साथ जाते हैं।हर कवि की विशिष्टता, संवेदनशीलता, पक्षधरता, दृष्टि, काव्य-प्रकृति, काव्य-भूमि, काव्य-चेतना ,काव्य-क्षमता,मूल पहचान को रेखांकित करना तथा कवि की काव्य-प्रविधि को समझना-समझाना आलोचक का अभिप्रेत रहा है। वे कवि की बेचैनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं।हिंदी कविता के ताप,उसकी कोमलता और सामथ्र्य से परिचित कराते हैं। इस तरह कविता विरोधी या कविता के वर्तमान परिदृश्य से निराश लोगों को जोरदार उत्तर देते हैं। वह समाज के यथार्थ से कविता में मौजूद यथार्थ की तुलना करते हैं जो उन्हें सही निष्कर्षों तक पहुँचाती है।
इस किताब की एक विशेषता यह है कि इसमें कविता पर ही नहीं अपने समय-समाज की गतिकी और काव्यशास्त्र पर भी बात की गई है।विभिन्न कवियों की कविताएं कैसी हैं पर तो जितेन्द्र की टिप्पणी है ही साथ ही एक अच्छी कविता और आलोचना कैसी होनी चाहिए ? बड़ी कविता कब सृजित होती है? किसी कविता के मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है? कोई कविता अपने पाठकों को कब बाँधती है? कला के संतुलित आग्रह और कलावादी होने में क्या अंतर है?बिना आवरण के समय का सच कविता में कैसे आता है? आदि प्रश्नों का भी वह जबाब देते हैं।
युवा आलोचक जितेन्द्र श्रीवास्तव आलोचना के दायित्व पर भी यत्र-तत्र अपनी राय व्यक्त करते चलते हैं। आज की कविता में समाजोन्मुखता की अभिधात्मक प्रस्तुति की वाहवाही के खतरे से आलोचना को सतर्क करते हैं। वे कहते हैं,‘‘ऐसे में होता यह है कि बहुत से आलोचक रचना में कहीं गहरे रचे-बसे यथार्थ को समझने-समझाने के बजाय उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे में कई बार अच्छी रचनाएं उचित व्याख्या से वंचित हो जाती हैं।’’
जितेन्द्र की आलोचना पद्धति की विशेषता है कि वह किसी भी कवि का मूल्यांकन उसकी जमीन से जोड़कर करते हैं।लोक और जनपद की जटिलताओं और समस्याओं की तलाश कविता में करते हैं। वह देखते हैं कि कवि की जड़ें अपनी जमीन में कितनी गहरी और फैली हुई हैं। उनका विश्वास है कि जो अपनी ‘मिट्टी-पानी और बानी’ से प्रेम नहीं करता समझिए वह किसी से प्रेम नहीं करता। कवि को उसके मुहावरे से पहचानने की कोशिश करते हैं। चेहरा विहीन समय में कवि के चेहरे की तलाश करते हैं। वह लोक के नाम पर बिदकने वाले आलोचकों में से नहीं हैं।वह इस बात को देखना जरूरी मानते हैं कि ‘‘कोई रचनाकार स्थानीयता को समझते हुए वैश्विक हो रहा है अथवा बिना किसी आधार के लगातार हवा में उड़ रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि आधारहीन वैश्विकता वायवीय होती है और कई बार मनुष्य विरोधी भी। किसी कवि के संदर्भ में स्थानीयता को चिह्नित करना इसलिए जरूरी होता है कि यह लक्षित किया जा सके कि उस कवि की ‘जमीन’ क्या है?’’ वह भाषायी शुद्धता के आग्रही नहीं हैं। लोक के शब्दों का प्रयोग उन्हें भाता है।लोक संदर्भों का स्वागत करते हैं। इसलिए हम पाते हैं कि जितेन्द्र किसी कवि की कविताओं पर लिखते हुए उसके अंचल का उल्लेख करना नहीं भूलते हैं। ‘लोक’ ‘लोक’ चिल्लाने वाली नहीं बल्कि ‘लोक’ में जो घट रहा है उस पर गहरी नजर रखने वाली कविता उनकी पसंद है। वह मानते हैं किसी कवि की स्थानीयता उसके द्वारा प्रयुक्त साक्ष्यों,प्रतीकों,बिंबों और शब्दों में प्रकट होती रहती है।
इस बात की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जितेन्द्र में अपने समकालीनों को पढ़ने,समझने और सराहने की पूरी उदारता है। अकुंठ भाव से उन पर लिखते हैं। युवा कविता को लेकर हमारे वरिष्ठ आलोचकों का जो निराशावादी और उदासीनता भरा भाव है उसको लक्ष्य करते हुए वह इस बात से इंकार करते हैं कि युवा कविता में नया कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने युवा कविता पर लिखे गए अपने लंबे आलेख ‘समय की आँख’ में लिखा है ,‘‘युवा कविता तो पूरे तेवर के साथ अपनी चमक बिखेर रही है।उसमें यदि लोकतत्व वाले कवि हैं तो नागर जीवन की बिडंबनाओं को अभिव्यक्त करने वाले भी। ये कवि बदलते गाँवों और बदलते शहरों के चरित्र तो पहचान ही रहे हैं,साथ ही अपने समय की सबसे बड़ी चुनौती बाजार को बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उससे उत्पन्न होने वाली त्रासदी बहुत प्रभावशाली ढंग से हिंदी कविता में आ रही है।.....ये कवि जीवन और समाज के उन कोने-अंतरों की ओर जाने का साहस रखते हैं,जिधर या तो पूर्ववर्ती गए नहीं हैं या बहुत कम गए हैं। इन युवा कवियों-कवयित्रियों की आवाज में बनावटी तल्खी नहीं है।’’ साथ ही वह इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करते कि कुछ युवा कवियों द्वारा कुछ वरिष्ठ कवियों की अंधाधुंध नकल की जा रही है। वह उन्हें सचेत करते है कि नए कवियों को यह समझना होगा और उससे जितनी जल्दी हो सके मुक्त होना होगा इसी से वह अपना मार्ग बनाने की ओर अग्रसर होंगे। वह इस बात की प्रशंसा करते हैं कि,’’ ‘दिल्ली’ के तमाम शोर के बावजूद अभी भी छोटे-छोटे कस्बों,गांवों और शहरों में रह रहे कवि लगातार सार्थक रच रहे हैं।..उन पर दिल्ली का कोई आतंक नहीं है और जिन पर है ,वे नष्ट हो रहे हैं।’’ दिल्ली में रहते हुए इस तरह दिल्ली का विरोध करना उनके साहस का परिचायक है।
आज आलोचना के सामने विश्वसनीयता का संकट है।प्रायोजित आलोचना ने उसके सामने इस संकट को खड़ा किया है। जितेन्द्र अपनी निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ आलोचना से इस परिदृश्य पर दमदार हस्तक्षेप करते हंै। अच्छी बात है कि वह किसी भी कवि पर लिखते हुए न किसी हड़बड़ी में दिखते हैं और न अतिरिक्त महत्व देने के अंदाज में। उनकी आलोचना कवि की पूरी संरचना का पता बता देती है। उनका यह कहना कि प्राणवान रचना यदि कंदराओं में भी पड़ी हो तो उन्हें ढूँढ जाना चाहिए। उनकी आलोचकीय प्रतिबद्धता और ईमानदारी का प्रमाण है। आज हिंदी साहित्य में विशेषकर कविता को ऐसे ही आलोचकों की आवश्यकता है क्योंकि आलोचना में जैसा भाई-भतीजावाद,गुटबाजी,मठबाजी,प्रायाजित आलोचना कार्यक्रम चल रहा है। उसके चलते जरूरी और अच्छी कविता बुरी कविता में खोती जा रही है। इस पुस्तक की खूबी है कि इसमें उन कोनों और हाशियों की ओर भी ध्यान दिया गया है जो अक्सर उपेक्षा के शिकार होते हैं। सत्ता केंद्रों से बाहर रचनारत कवियों पर भी पूरी नजर डाली गई है।फलस्वरूप कुछ कम चर्चित कवियों की भी चर्चा यहाँ हुई है बावजूद इसके, कुछ चर्चित वरिष्ठ और युवा कवि छूट गए हैं जो थोड़ा खटकता है।
जितेन्द्र की आलोचना एकेडमिक बोझ से दबी हुई नहीं है। भाषा आम पाठक के अनुकूल है।उनकी भाषा में पंडिताऊपन और ऊबाउपन नहीं है। वह पाठक को उलझाते नहीं बल्कि कविता के मर्म तक पहुँचने में उसकी मदद करते हैं।पूरे समय और समाज की आलोचना करते हैं। इसका परिणाम यह है कि उनकी आलोचना कविता के प्रति अनुराग पैदा करने के साथ-साथ जीवन के प्रति भी अनुराग पैदा करती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद समकालीनल हिंदी कविता पर उनसे आगे और अधिक गहराई और विस्तार से विश्लेषण की अपेक्षा बढ़ गई है।यह किताब निश्चित रूप से हिंदी कविता पर बातचीत के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगी।
***
विचारधारा नए विमर्श और समकालीन कविता: जितेन्द्र श्रीवास्तव
प्रकाशकः किताबघर प्रकाशन नई दिल्ली।
मूल्यःपाँच सौ रुपए।
***
संपर्कः महेश चंद्र पुनेठा शिव कालोनी पियाना वार्ड पो-डिग्री कालेज जिला- पिथौरागढ़ पिन- 262501 (उत्तराखंड)
मोबाइल: 09411707470